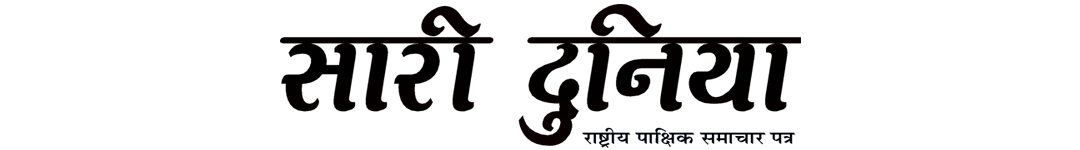– नासिरूद्दीन
हर तरफ़ नफ़रत का शोर है। नफ़रत सड़कों पर, ट्रेनों में, मोहल्लों में, महानगरों में हिंसा के रूप में दिख रही है। नफ़रत बाज़ार में भी पसर रही है। कहीं वेशभूषा तो कहीं हलाल और झटका का शोर है। बहुत सारे लोगों को लगा था कि व्हाट्सएप और टेलीविज़न पर दिन-रात चलने वाली हिन्दू-मुसलमान बहस, सोशल मीडिया और टीवी तक ही सीमित रहेगी,पर ऐसा हुआ नहीं।
नफ़रत के लिए सिर्फ़ टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार ठहरा देना, उन बातों से आँख चुराना होगा, जो इनकी जड़ों में है। नफ़रत, महज़ व्यक्ति की व्यक्ति से नहीं है. यह सामूहिक और सामुदायिक नफ़रत है। यह राजनीतिक विचार है। इसे बढ़ाने और पनपाने में उन लोगों की असल भूमिका है, जो अलग-अलग सत्ता की जगहों पर हैं।
ऐसे में कई बार ऐसा अहसास होता है कि हम चारों ओर नफ़रत से घिर चुके हैं। ख़ासकर मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय माहौल में यह ज़्यादा अहसास होता है। …और मीडिया और सोशल मीडिया पर यह अहसास और बढ़ जाता है।
पिछले दिनों नफ़रत और हिंसा पर एक टिप्पणी के बाद कई सारे दोस्तों ने अपनी कुछ प्रतिक्रियाएँ भेजीं। कुछ ने अपने अनुभव साझा किए। ये अनुभव बताते हैं कि हम साझेपन में कैसे रहते आए हैं और आज भी कैसे रह रहे हैं। ये अनुभव हमें आज के हालात के बारे में, अपने बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये इस हालात से निकलने में भी मदद कर सकते हैं।
1. तीर्थयात्रा के कपड़े मुसलमान ने सीए
अनुराग पत्रकार रहे हैं। अब बिजनेस करते हैं। आपसी नफ़रत बढ़ने पर उनकी राय है, जो हो रहा है, वह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता नहीं। मेरे गाँव में दो-तीन मुसलमान परिवार ही होंगे। इनमें से एक दर्ज़ी का काम करते हैं। अभी मेरे पिता जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने ही पूरे कपड़े सी कर दिए। कभी कोई बात नहीं हुई। मैं उनकी बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से उनकी दुकान पर बैठता रहा हूँ।
अभी हाल में मैंने एक नया काम शुरू किया है। हमने जो फैक्ट्री किराए पर ली है, वह एक मुसलमान की है। पहले ये फैक्ट्री उनके रिश्तेदार चलाते थे। अब मैं और मेरे मित्र ज्ञान मिलकर चला रहे हैं। सवाल वही है, ये कौन लोग हैं जिनमें एक-दूसरे के लिए इतनी नफरत है।
2. हिन्दू-मुसलमान नहीं, इंसान की फ़ितरत देखें
प्रगीत शर्मा राजस्थान के रहने वाले हैं। इंजीनियर बनने की पढ़ाई की। अपने मन का काम करना था तो ख़ुद का काम शुरू किया – हैंडमेड फैशन ज्वेलरी के एक्सपोर्ट का। उनका व्यापार मुसलमानों के इर्द-गिर्द ही खड़ा हुआ। वे बताते हैं, जिस दादरी में अख़लाक़ की हत्या हो गई थी, उसके पास के एक गाँव से मेरा वास्ता है। मेरी साथ काम करने वाले सभी कलाकार-दस्तकार मुसलमान हैं। हालाँकि, न तो मैं उन्हें मुसलमान के रूप में देखता हूँ और न वे मुझे विधर्मी के रूप में। उनका हुनर, आपसी भरोसा और यक़ीन ही हमारे रिश्ते का आधार है। बड़ी संख्या में गाँव की लड़कियाँ इस काम से जुड़ी हैं। कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। यही नहीं, रिश्ते का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उनके बीच कोई आपसी विवाद होता है या उनकी निजी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो वे पहले मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं उनके लिए भाई साहब हूँ। यही नहीं, एक बार की बात है। ऑर्डर बाहर जाना था। काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो सबने मिलकर ईद के दिन भी काम पूरा किया। अगर उन्हें काम मिल रहा है तो मैं भी आज जो हूँ, उनकी वजह से ही हूँ।
मेरे इस भरोसे और यक़ीन को अक़सर चुनौती दी गई। कई नज़दीकी कहते हैं, कि इन पर इतना भरोसा ठीक नहीं। धोखा खाओगे। एक क़िस्सा बताता हूँ। जब मेरा उस गाँव से रिश्ता मज़बूत हुआ तो दोस्तों के लाख मना करने के बावजूद मैंने वहीं एक ज़मीन भी ख़रीद ली। मैं नोएडा में रहता हूँ। एक दिन अचानक मेरे पास ख़बर आई कि मेरी ज़मीन पर हंगामा हो रहा है। एक तरफ़ हिन्दू खड़े हैं और दूसरी तरफ़ मुसलमान। हिंसा की हालत बन रही है। जब पड़ताल की तो पता चला कि मेरी ज़मीन से सटे एक साहब की ज़मीन है। उन्होंने अपना खेत जोतते हुए मेरी ज़मीन के कुछ हिस्से भी जोत दिए। जब गाँव के एक व्यक्ति ने देखा तो उसने टोका। उन्होंने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या यह तुम्हारी ज़मीन है? और वे कौन सा देखने आ रहे हैं? इस बीच और गाँव वाले भी जुट गए। उन्होंने कहा कि यह भाई साहब की ज़मीन है, हम जोतने नहीं देंगे। काफ़ी हंगामें के बाद मेरी ज़मीन बची। जोतने वाले को आप हिन्दू कह सकते हैं और बचाने वाले को मुसलमान। लेकिन मेरा मानना है कि अच्छाई-बुराई इंसानी फ़ितरत है। इसका धर्म से लेना देना नहीं है। इंसान, इंसान ही रहता है.. हम उसे हिन्दू-मुसलमान के रूप में देखते हैं। हम यही नहीं समझना चाहते।
3. एक थे हमारे रज्जाक चाचा
आजमगढ़ के बिलारी बढ़या के राजदेव चतुर्वेदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे अपना अनुभव सुनाते हैं, मेरे बचपन की बात है। हमारे गाँव में केवल एक मुसलमान परिवार था। इसके मुखिया दरगाही बाबा थे। आजीविका का साधन खेती-बाड़ी थी। कभी-कभी वे गाँव के मांसाहारी परिवारों के लिए बकरे काट कर भी बेचते थे। उनके एक अनाथ रिश्तेदार रज्जाक, साथ में ही रहते थे। हम ब्राह्मण माने जाने वाले परिवार से थे, पिता जी पुरोहिती का काम भी करते थे। हम और हमारी बड़ी बहन छोटे थे। पिता जी ने रज्जाक को हम लोगों की देखभाल के लिए अपने पास रख लिया। वे घर के दूसरे काम भी करते थे। वे हमारी माँ को भौजी और बाबू को भइया कहते थे। इसलिए अब वे हमारे रज्जाक चाचा हो गए थे। माँ बताती थीं कि रज्जाक चाचा पिता जी के साथ ही भोजन करते थे। यदि पिता जी को भोजन करने मे देर होती तो रज्जाक चाचा भी खाना खाने से मना कर देते थे। कहते कि भइया आ जाएँगे और जब भगवान का भोग लग जाएगा, उसके बाद ही साथ में भोजन करूँगा। बाद में वे कहीं चले गए।
इधर दरगाही बाबा के एक लड़के सुक्खु थे। वे हमारे पिता जी को बड़का बाबू और माँ को बडकी माई ही कहते थे। सुक्खु दादा के तीन लड़के हैं। एक बेटा शब्बीर गाँव में ही रहता है। आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। हमारे घर से अच्छे संबंध हैं, घर पास में ही है। रोज सुबह-शाम मिलना होता है। हमें बड़का भइया और पत्नी को बड़की भौजी कहते हैं। हमारी पत्नी और बेटियों को शब्बीर के बच्चों का बड़ा ख्याल रहता है, हमारे गाँव में तो उनसे किसी को परेशानी नहीं है।
4. दामाद जी से पान के पैसे कैसे ले सकते थे हाशिम
दीपक ढोलकिया 75 साल के हैं। लम्बे अरसे तक आकाशवाणी के समाचार प्रभाग से जुड़े रहे। वे दो क़िस्से बताते हैं –
बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के नानपारा से मेरी सास मनोरमा जी को दिल्ली आना था। घर के बरामदे से उन्होंने किसी को आवाज़ दी कि रिक्शा भेज दे। रिक्शा आया नहीं तो वह गली में आ गई। बाहर सड़क पर देखा तो एक ओर मुसलमानों का हुजूम खड़ा था और दूसरी ओर हिंदुओं का। उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है? इनमें कई चेहरे जाने पहचाने थे। इतने में मुसलमान भीड़ में से एक लड़का उनके पास आया। बोला, ‘अम्मा जी, यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाइए घर में…’ उसकी आवाज में अपनेपन की डाँट थी। मनोरमा जी ने कहा कि ‘बेटे मुझे बस पकड़नी है और रिक्शा नहीं आ रहा।’ लड़के ने कहा कि ऐसे में रिक्शा वाला यहाँ कैसे आएगा? आप रुकिए, मैं लाता हूँ। वह थोड़ी देर में रिक्शा ले कर आया। अम्मा जी ने बैठते हुए पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़का भड़क कर बोला, ‘अम्मा जी, हिन्दुओं ने हमारी मस्जिद गिरा दी है। हम भी बरादाश्त नहीं करेंगे।’ फिर उसने रिक्शे वाले को कहा पीछे की गली से अम्मा जी को बस स्टेशन पहुँचा दो। इधर रिक्शा मुड़ रहा था और लड़का मुसलमानों के हुजूम में शामिल हो गया। वैसे, नानपारा में कुछ नहीं हुआ।
एक हाशिम थे। उनका पान आपने खाया नहीं है। मैंने खाए हैं। मुझ दामाद जी के पान के पैसे कैसे लेता? कभी नहीं लिए। विरोध में शामिल होने के लिए उसने भी दुकान बंद रखी थी। दोनों ओर से भीड़ छँट गई। हाशिम ने फिर से दुकान खोल ली।
आज नानपारा में कोई नहीं है। मेरी पत्नी का पुश्तैनी घर भी बिक चुका है। लेकिन मेरी इच्छा होती है कि नानपारा जाऊँ। जानूँ कि क्या मैं उसी नानपारा में वापस आया हूँ या कोई नया नानपारा है?
5. काश! मेरा वह भारत कहीं मिल जाए
दीपक ढोलकिया एक और क़िस्सा सुनाते हैं –
साल 2000 में मेरी बेटी वड़ोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में एमएससी करने के लिए गई। मैं दाख़िला दिलवा कर दिल्ली वापस आ रहा था। बेटी स्टेशन पर छोड़ने आई। ट्रेन चलने लगी तब वह रोने लगी। ट्रेन ने गति पकड़ी और बेटी नज़र से दूर हो गई। मैंने फ़ौरन ही किताब खोली। उसमें अपना चेहरा छुपा लिया।
मेरे कंपार्टमेंट में 50–55 की उम्र की चार महिलाएँ थीं। वे एक सत्संग से वापस आ रही थीं। ट्रेन खुलते ही उन्होंने जोर-जोर से भजन शुरू कर दिए। एकाध घंटे के बाद उन्होंने धुन शुरू कर दी – राम एक…राम दो…राम नब्बे…राम 108… इसके बाद मालाएँ निकालीं। मनके फेरने लगीं। डिब्बे में शांति हो गई।
लेकिन पाँच-सात मिनट में ही एक फ़कीर अल्लाह के नाम की दुहाई देता हुआ आ गया। फ़कीर देख नहीं सकता था। किसी ने उसे खाना दिया तो किसी ने पैसे। वह खड़ा रहा और बोलता रहा। उसे उम्मीद थी कि डिब्बे में अभी दाता लोग बचे होंगे।
एक महिला ने माला फेरते हुए एक आँख खोली और मुझे कोहनी मारी। मैंने उसकी ओर देखा तो उसने अपना पर्स खोला और एक रुपया निकाला। मेरे हाथ में सिक्का रखा। फकीर को देने का इशारा किया। उसके साथ तीन आँखें और खुलीं। तीन बटुए और खुले। हर एक में से एक का सिक्का निकला। मैं समझ गया था कि ये तीन सिक्के भी मुझे फकीर को देने हैं। फकीर चला गया। वे माला फेरने लगीं। डिब्बे में फिर शांति हो गई।
मेरे लिए यह शांति कुछ और थी। मैंने किताब रख दी। सोचने लगा – यह है मेरा भारत… राम के नाम की माला जपने वाली महिलाओं के लिए फकीर भी वही था, जो वे स्वयं थीं। होठों पर नाम एक हिन्दू भगवान का, और दान अल्लाह वाले को!
मुझे लगा कि मेरी अनास्था बहुत तुच्छ है। इनकी छोटी आस्थाएँ, मेरी अनास्था से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, आम आदमी के मन में कोई ज़हर नहीं है।
गुजरात के दंगे इसके बाद हुए। उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ और होता है। मेरा विश्वास डगमगाने लगा है कि जिस भारत को मैंने वड़ोदरा से दिल्ली आने वाली ट्रेन में देखा था, वही क्या आज भी है? चाहता हूँ कि वह भारत कहीं मिल जाए।
– नासिरूद्दीन
(साभार : नवजीवन। यह आलेख ‘संडे नवजीवन’ के 20 अगस्त 2023 के अंक में छपा है। आख़िरी कहानी अख़बार में नहीं छपी है।)