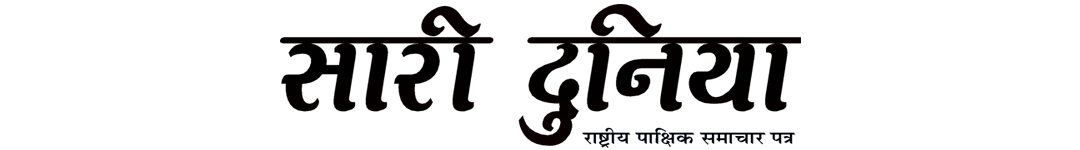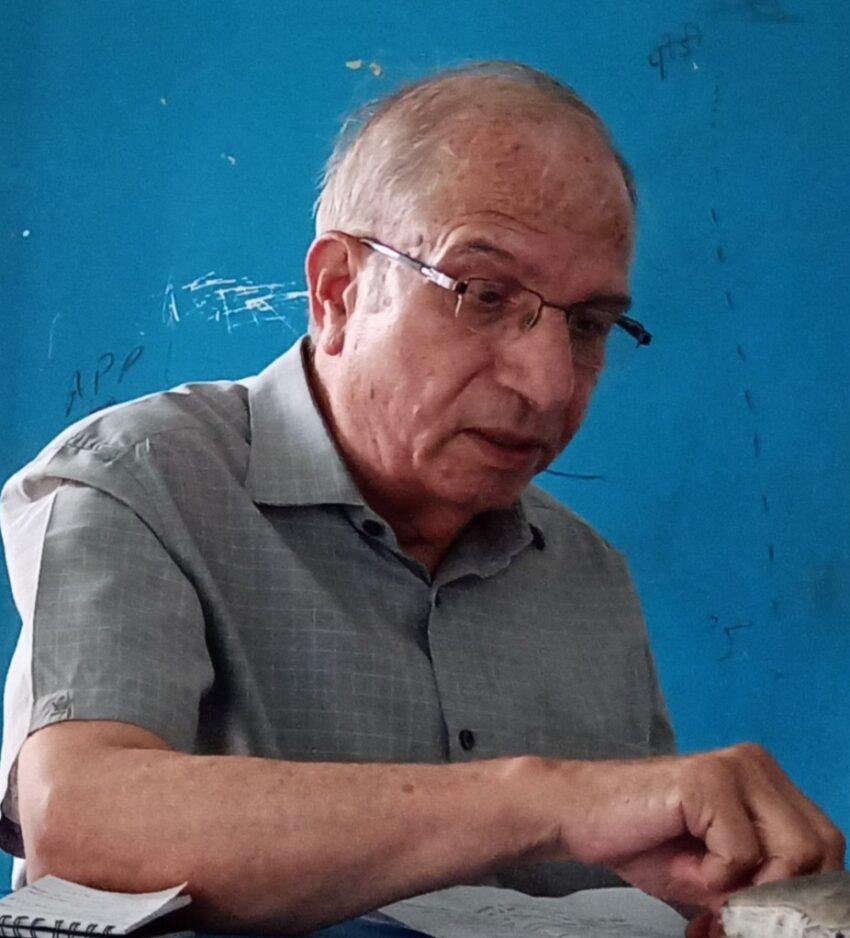लेखक – सुरेंद्र कुमार
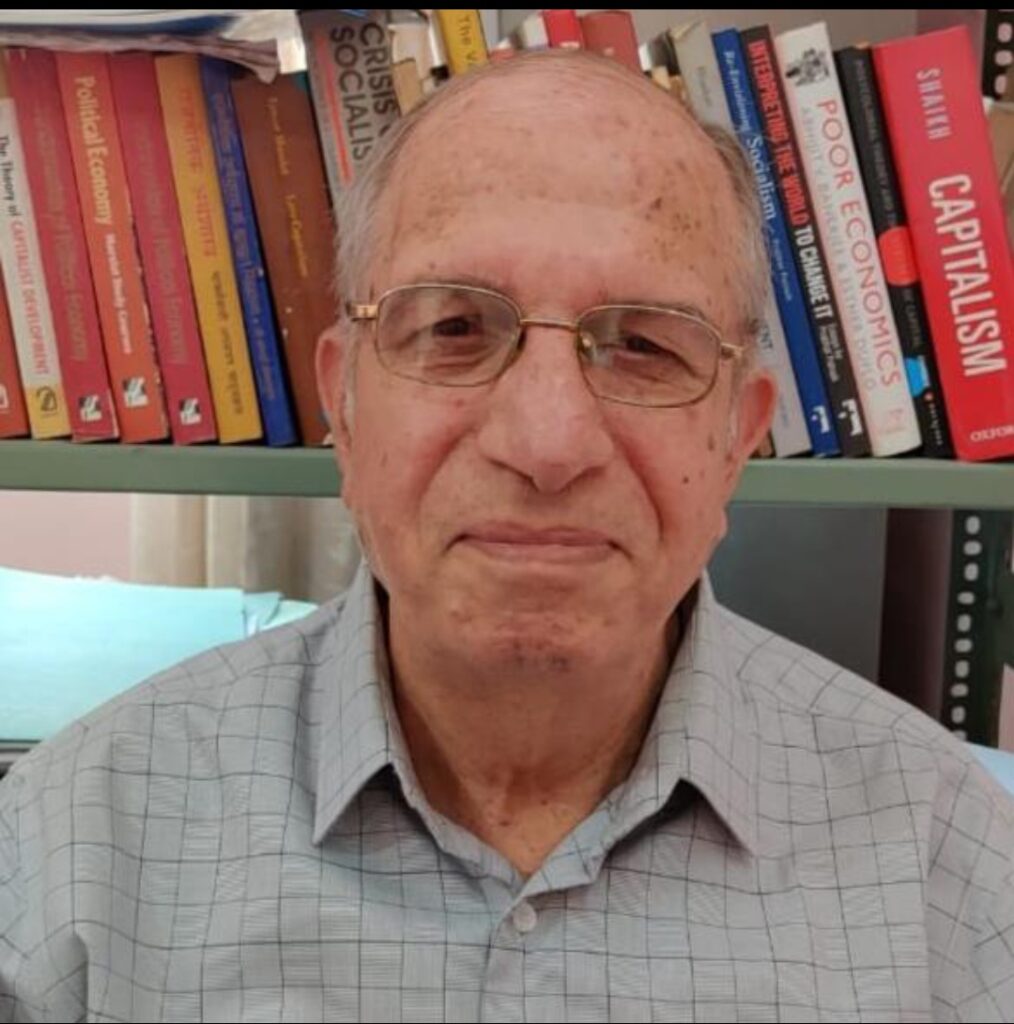
मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति और आलोचनात्मक मानसिकता (critical thinking) का विकास क़ैसे किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर लाख टके का है! दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है उसे जानने की जिज्ञासा मनुष्य की सामान्य प्रकृति है। घटना/प्रक्रिया को जानने के बाद उसे समझने का प्रयास करना और हो सके तो उसका व्यक्तिगत, पारिवारिक, और सामाजिक हितों में प्रयोग करना भी व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति/प्रकृति है। समय के साथ-साथ विभिन्न घटनाओं को जानने, पहचानने और समझने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से हर बच्चे के सोचने-समझने के तरीके का विकास होता है। इस सोचने-समझने की शैली को व्यक्ति की मानसिकता/सोच कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, मानसिकता या सोच एक व्यक्ति की वह मनोवृत्ति है जो उस व्यक्ति के इस दुनिया को देखने-समझने के दृष्टिकोण और व्यवहार को विशेष आकार देती है या साकार करती है।
मनुष्य जो भी देखता है, उसे समझने के लिए, उसके बारे में अपने आप से प्रश्न करता है : यह क्या है, क्यों और कैसे ऐसा है? बच्चे की पहली पाठशाला बच्चे के मां-बाप, और परिवार हैं। बचपन में बच्चे के संस्कारों का निर्माण उसके मानस पर अविस्मरणीय/अमित छाप छोड़ता है जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। बचपन के संस्कारों में अनेक बातें/समस्याएं बिना सुलझे रह जाती हैं। इन्हें बच्चा, परिवार या समाज में व्याप्त संस्थागत पुराने (रूढ़िवादी) विचारों और कुछ हद तक अंधविश्वासों पर विश्वास या किसी अलौकिक शक्ति/भगवान पर आस्था के सहारे समझता है और अपने मन की उलझन/संशय को दूर करने का प्रयास करता है। इस दुनिया की सभी चीज़ों को भगवान ने बनाया है, इस विश्वास से उस के मानस में अलौकिक शक्तियों में आस्था गहरी होती जाती है। बहुत बार अलौकिक शक्तियों में आस्था, बचपन में जिज्ञासा से उत्पन्न प्रश्नों ‘क्या’,’क्यों’ और ‘कैसे’, जैसे मन में उठने वाले सवालों को कुछ हद तक अवरुद्ध कर देते हैं और अपने बड़ों से सुनी-सुनाई बातें (मुहल्ले में चर्चाएं) उन के ज्ञान का मुख्य स्रोत बन जाती हैं। यह एक सुविधापूर्ण धारणा है कि जो हो रहा है वह भगवान द्वारा रचित है। प्रायः यदि परिवार या आसपास पढ़े-लिखे (या ज्ञानवान) लोग हैं जो बच्चे से वार्तालाप में बातों या घटनाओं की व्याख्या करते हैं तो बच्चे की सोच का विकास थोड़ा बहुत तर्कशील या विवेकपूर्ण होता है। प्रायः यदि परिवार में पढ़े-लिखे लोग नहीं है, तो बड़े-बूढ़े अपने विवेक और कुछ रूढ़िवादी समझ से बच्चे की सोच को अधिक प्रभावित करते हैं। बच्चे के आसपास का वातावरण भी उसकी सोच-समझ को प्रभावित करता है।
बच्चे की घर से अगली पाठशाला बच्चे का स्कूल है जिसमें अध्यापक पुस्तकों की सहायता से बच्चे को पढ़ना-लिखना और सोचना सिखाते हैं। आगे की कक्षाओं में भाषा ज्ञान के साथ-साथ सामान्य सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और गणित की शिक्षा भी दी जाती है। इस प्रक्रिया में बच्चे के ज्ञान और सोचने की क्षमता का विकास होता है। ऐसा तो नहीं कि जिन तथ्यों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उन्हें वह अपनी स्मरण शक्ति से याद कर के परीक्षा में दोहराकर परीक्षा को पास कर ले और समझ का विकास कम ही हो! हमारे देश में, सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चे के सामान्य ज्ञान के साथ-साथ आलोचनात्मक सोच/ज्ञान (क्या, क्यों और कैसे का उत्तर) का कितना विकास होता है, यह एक विचारणीय विषय है।
आलोचनात्मक मानसिकता :
तार्किक सोच से हमारा भाव है कि बिना किसी पक्षपात के, निष्पक्ष होकर, वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना और निष्कर्ष निकालना। आलोचनात्मक मानसिकता का अर्थ मात्र गलतियां निकालना नहीं है। इससे हमारा भाव है कि तर्क के आधार पर सोचने-विचारने और दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता का विकास। आलोचनात्मक मानसिकता के तर्कशक्ति के साथ-साथ दो और पहलू हैं : (अ) व्यक्ति की विश्व दृष्टि या दुनिया के बारे में दृष्टिकोण और (ब) व्यक्ति निष्पक्ष भाव के साथ न्यायालय में एक जज की तरह नैतिक मूल्यों या उस बौद्धिक प्रक्रिया को अपनाए जिससे सच्चाई के जितना हो सके निकट पहुंचे। आलोचनात्मक मानसिकता के तीन अनिवार्य तत्त्व हैं : (i) तर्क क्षमता, (ii) विश्व दृष्टि और (iii) निष्पक्ष भाव से सच्चाई तक पहुंचने की बौद्धिक प्रक्रिया। आलोचनात्मक मानसिकता का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति संदेहवादी नहीं है, यानी हर बात पर अपने आप से ‘किंतु’-‘परंतु’ नहीं करता।
तर्क क्षमता के विभिन्न पक्ष :
संज्ञान प्रक्रिया से हमारा भाव है, मनुष्य की अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की सूचनाएं एकत्रित करके दुनिया को समझने की प्रक्रिया। तर्क क्षमता/शक्ति का अर्थ है कि मनुष्य अपनी सोचने-समझने की क्षमता का उपयोग करके सूचनाओं का विश्लेषण करे। तर्क के आधार पर सोचने में निपुणता साधारण से ऊपर की/उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को केवल आत्मसात् करने की बजाय प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना, उन निष्कर्षों का विश्लेषण करना, उनकी व्याख्या करना, उनका मूल्यांकन करना या उन तर्कों में कमियां निकालना आदि शामिल हैं।
अनुभव बताता है कि सतत् प्रयत्न से तर्क क्षमता का विकास करके उसमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है। एक मनुष्य में तर्कशील सोच का विकास करना अपेक्षाकृत आसान काम है। ऐसा भी सम्भव है कि एक व्यक्ति की तर्क शक्ति का विकास तो अपेक्षाकृत अधिक हो गया हो परंतु उस के दुनिया के बारे में दृष्टिकोण और जीवन के मूल्यों का विकास में कमियां रह गई हों। अधिक विकसित आलोचनात्मक सोच (जिसमें विश्व दृष्टि और जीवन मूल्यों का समावेश हो) की परिकल्पना करना और उसे किसी व्यक्ति में विकसित करना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। आलोचनात्मक मानसिकता के दूसरे दोनों तत्त्व और अधिक चुनौतीपूर्ण हैं।
विश्व दृष्टि (दुनिया को देखने का नज़रिया) के आयाम :
समाज शास्त्र की एक मौलिक सच्चाई यह है कि दुनिया प्रायः ऐसी नहीं होती जैसी पहली दृष्टि में दिखाई देती है। इसे हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझने का यत्न करना होगा। हमारा सामाजिक परिवेश हमारी सोच को प्रभावित/सीमित करता है। समाज में जो भूमिका हम अदा करते हैं ,वह भी हमारे व्यवहार और हमारी सामाजिक पहचान को प्रभावित करती है। हम अपनी अज्ञानता से अनभिज्ञ होते हैं और आंशिक सत्य को ही पूरा सच मान लेते हैं। आंशिक सच, एकदम झूठ की तरह, हमें सच्चाई से भटका सकता है। इसलिए आलोचनात्मक सोच का व्यक्ति बातों को उनकी फ़ेस वैल्यू/अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमें दुनिया को देखने का नज़रिया तर्कपूर्ण समझ के आधार पर बनाना चाहिए, जिससे सच्चाई के विभिन्न पक्षों को उनके पूरे कद में जान सकें या समझ सकें।
नैतिकता के साथ सच्चाई/वस्तिकता तक पहुंचने की बौद्धिक प्रक्रिया :
व्यक्ति, नैतिक मूल्यों (ठीक और गलत का विवेक) के साथ न्यायालय में एक जज की तरह उस निष्पक्ष बौद्धिक प्रक्रिया को अपनाए जिससे सच्चाई के जितना हो सके, निकट पहुंचे। सच्चाई को जानने के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निष्पक्ष भाव से नैतिक प्रतिबद्धता और जीवन मूल्य होने चाहिए। संगठित तर्कहीनता (organised irrationality) के विरुद्ध, संदेहवादी सोच तर्क शक्ति का एक बहुत बड़ा हथियार है। तर्कशील सोच समाज के विकास का एक बहुत बड़ा संसाधन है।
यदि बहुआयामी (अनेक पक्षीय) आलोचनात्मक सोच के सामाजिक लाभ इतने अधिक हैं तो समाज में इस तरह की सोच का विकास करना हमारा कर्तव्य है। क्या भौतिक विज्ञान इस प्रकार की सोच विकसित करने में कारगर है? देखा गया है कि यह ज़रूरी नहीं है। ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक ज्ञान और अंधविश्वासों के प्रति आस्था में सम्बंध काफ़ी कमज़ोर है, अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ वैज्ञानिक नियमों का ज्ञान है तो उस की अंधविश्वासों पर आस्था बिल्कुल खत्म हो जाए। अनेक समाजशास्त्रियों का निष्कर्ष है कि हम स्कूल-कॉलेज में विज्ञान के शिक्षण में, कुछ वैज्ञानिक तथ्यों और उस के सिद्धांतो को पढ़ते-पढ़ाते हैं, न कि दुनिया को समझने के समग्र नियमों को, यानी व्यक्ति की हर विषय/समस्या को तर्कपूर्ण ढंग से समझने की क्षमता का विकास नहीं होता, जिस कारण आलोचनात्मक सोच का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पता। आलोचनात्मक सोच वैज्ञानिक सोच का वह नियम जो जीवन के हर पहलू/पक्ष को विश्लेषणात्मक ढंग से समझने की क्षमता उत्पन्न करने में सहायता करता है।
मनुष्य के सामाजिक जीवन में यदि अंधविश्वासों ने हमारी मानसिकता को जकड़ रखा है तो इसका अर्थ है कि एक बच्चे की कक्षा में विज्ञान की शिक्षा इस जकड़न को तोड़ने में काफ़ी कमज़ोर साबित हुई है। इस जकड़न को तोड़ने के लिए बहुआयामी आलोचनात्मक सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। यह संदेहास्पद है कि कक्षा में और अपनी पाठ्य पुस्तकों से बच्चा जो ज्ञान अर्जित करता है, उससे सच्चाई जानने के लिए उसकी विश्व दृष्टि और जीवन मूल्य किस हद तक प्रभावित होते हैं। बहुत-से अध्यापक और पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की सोच बहुआयामी और आलोचनात्मक नहीं है और वे संकुचित दायरे में रहकर पठन-पाठन का कार्य करते हैं। इस प्रकार के अध्यापन से केवल अर्ध-आलोचनात्मक सोच का ही विकास होता है।
यदि हम सोचते हैं कि वर्तमान में जिस ढंग से हम सामान्य शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की शिक्षा देते हैं, उससे बहुपक्षीय आलोचनात्मक सोच का विकास हो ही जाएगा तो यह गलतफ़हमी होगी और केवल सामान्य समझ होगी। आलोचनात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए हमें बहुआयामी आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना होगा जिसमें सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष को छोड़े बिना तर्कशक्ति का विकास हो और संशययुक्त विश्व दृष्टि के साथ-साथ एक न्यायप्रिय न्यायधीश/जज के जीवन-मूल्यों का भी विकास हो। सामान्य भाषा में तर्कपूर्ण सोच और वैज्ञानिक सोच को पर्यायवाची मान लिया जाता है।
एक बच्चे में आलोचनात्मक मानसिकता के विकास के लिए अध्यापकों को पुरज़ोर प्रयास करना होगा ताकि आगे चलकर उसकी वैज्ञानिक सोच का विकास किया जा सके।
(यह लेख आंशिक रूप से हावर्ड गबेंनेसच के लेख ‘आलोचनात्मक सोच’, स्केप्टिकल इंक्वाइरर, मार्च-अप्रैल, 2006 पर आधारित है।)
(प्रोफ़ेसर सुरेंद्र कुमार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और शैक्षणिक मामलों के डीन रहे हैं।)
e-mail id: ksurin@rediffmail.com,
M: 8005492943
कृपया अपने सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ हमें यहाँ मेल करें: ksurin@rediffmail.com, saridunianews@gmail.com,
avi99sh@gmail.com