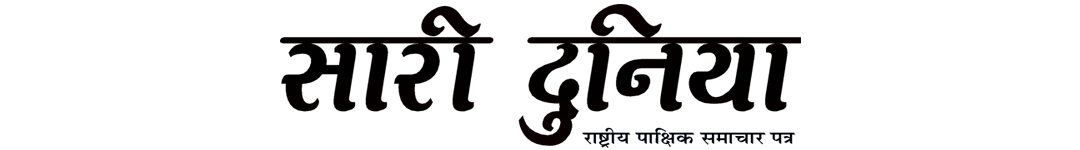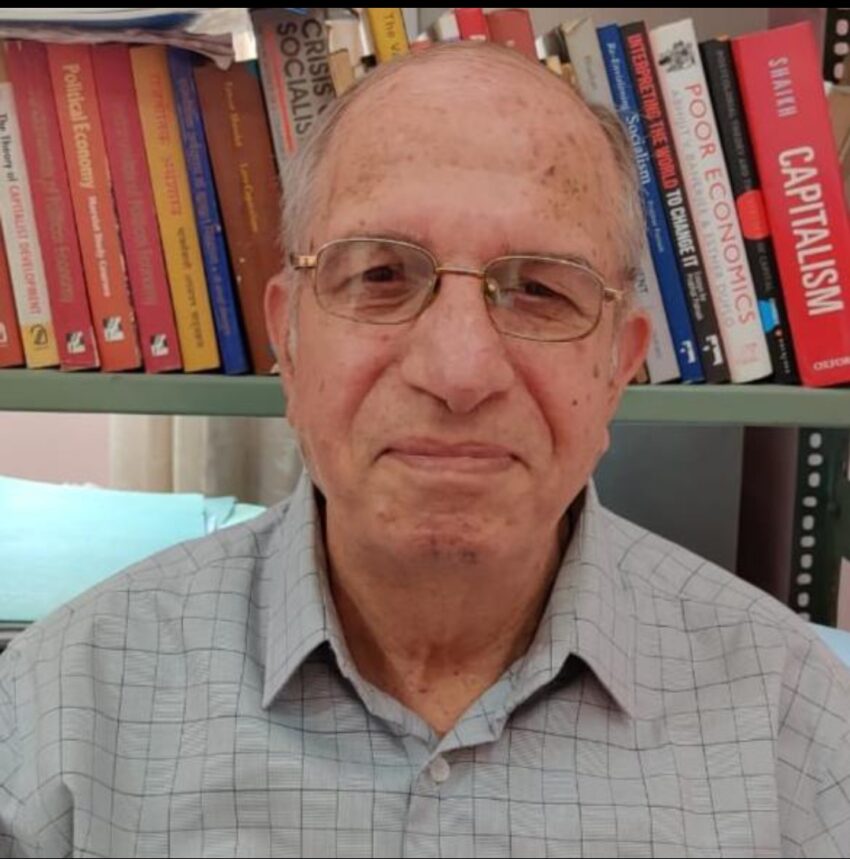लेखक – प्रोफ़ेसर सुरेंद्र कुमार
वैज्ञानिक प्रक्रिया, सोचने समझने की वह विधि है जिस में हम किसी भी घटना और उस के सम्भावित कारणों में वह सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिस से उस घटना की व्याख्या की जा सके। ये सम्भावित कारण इस भौतिक़ संसार में ही विद्यमान होते हैं, किसी अलौकिक शक्ति के प्रभावस्वरूप नहीं। अलौकिक शक्ति में विश्वास आस्था का प्रश्न है और विज्ञान प्रमाण के बिना आस्था को स्वीकार नहीं करता। प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए प्रयोग की जाने वाली इस विधि को हम वैज्ञानिक पद्धति/प्रक्रिया कह सकते हैं।
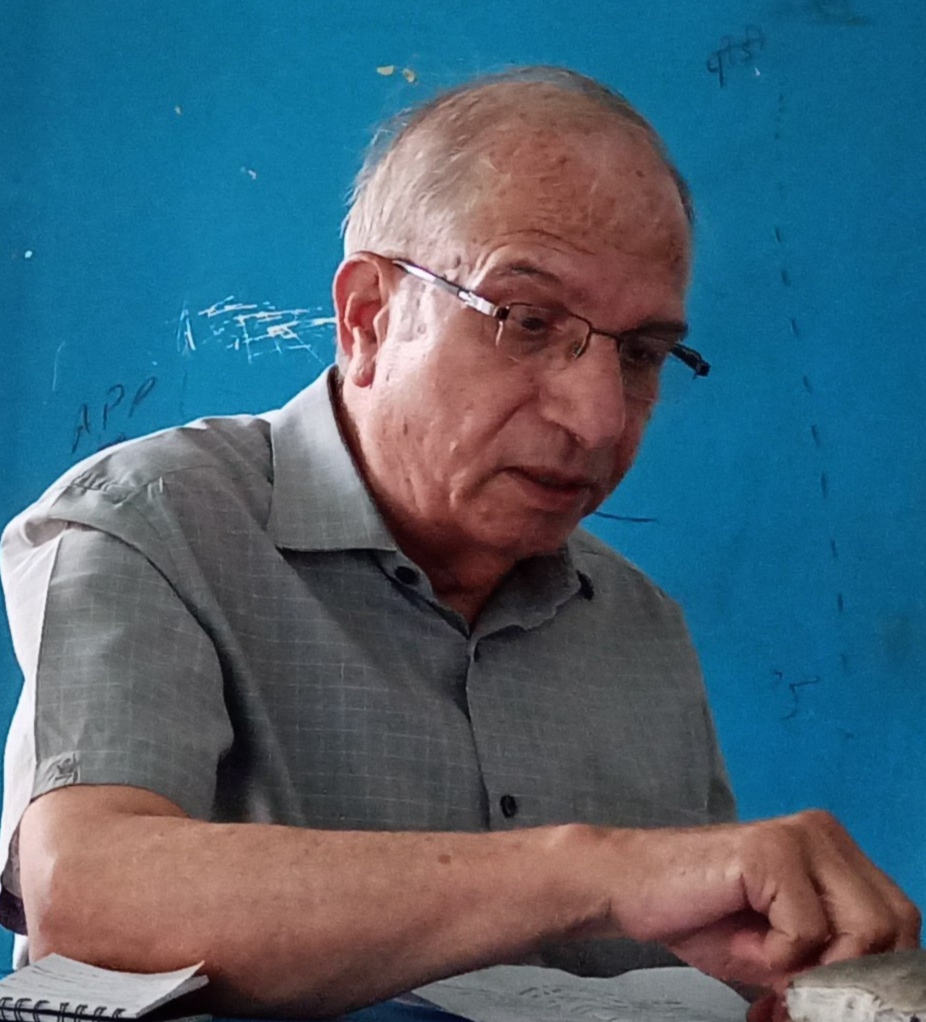
जब हम दुनिया में कुछ भी घटित होता देखते हैं तो मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। जैसे क्या हो रहा है? क्यों और कैसे हो रहा है? जिज्ञासावश, मनुष्य इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है। यह मानव का स्वभाव है। आइए, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें जो इस दौरान हमारे चेतन और अचेतन मन में चलती है।
क्या हो रहा है, यह जानने के लिए मनुष्य अपनी ज्ञानेन्द्रियों (आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा) की सहायता से स्वभावत: अपने आस-पास की दुनिया से तथ्य इकट्ठे करता है। उन तथ्यों को समझने के लिए हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव (Question-Answer) पैदा होते हैं। क्या है, क्यों और कैसे है? इस कारण से तो ऐसा नहीं हो रहा है या उस कारण से तो नहीं? इन भावों में से जो भाव हम तथ्यों के अनुरूप पाते हैं, उस भाव को पहली परिकल्पना या सम्भव व्याख्या कहा जा सकता है। यदि यह परिकल्पना बाद में हमारे सामने आने वाले तथ्यों की व्याख्या कर देती है तब तो ठीक है, वरना उस परिकल्पना में उचित संशोधन कर या वैकल्पिक परिकल्पना की सहायता से हम दोबारा तथ्यों की व्याख्या करने का यत्न करते हैं।
यह प्रक्रिया हमारे चेतन-अचेतन मन में तब तक जारी रहती है जब तक हम उस परिकल्पना तक नहीं पहुँच जाते जिस से काफ़ी हद तक हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। उदाहरण के लिए, आकाश पर सूर्य और तारों/ग्रहों को घूमता देख कर मनुष्य ने पहली परिकल्पना बनाई कि सूर्य और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। इसी परिकल्पना के आधार पर खगोल-विज्ञान (astronomy) और ज्योतिष-शास्त्र (astrology) का विकास किया गया। धर्मशास्त्रों में भी इसी परिकल्पना को मान्यता मिली। लेकिन जब इस परिकल्पना से खगोल की अनेक प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं हो सकी तो नयी परिकल्पना गढ़ी गई कि पृथ्वी सूर्य के चारों और घूमती है। दुनिया के धार्मिक गुरुओं और ज्योतिष शास्त्रियों ने इस नयी परिकल्पना को धार्मिक आस्था के विरुद्ध बताया और इस का ज़बरदस्त विरोध किया। इसी के चलते उस समय के वैज्ञानिकों को अनेक यातनाएँ झेलनी पड़ीं। लेकिन इस नयी परिकल्पना से कि धरती सूर्य के चारों और घूमती है, ब्रह्माण्ड की कई प्रक्रियाओं की सुचारु रूप से व्याख्या हो पाई और अन्त में सभी को स्वीकार करना पड़ा कि पृथ्वी सूर्य के चारों और घूमती है।
परिकल्पनाओं को व्यापक स्तर पर स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण और समझने लायक़ है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ही लें तो धरती द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने की अवधारणा का उस समय की धार्मिक-राजनैतिक व्यवस्था द्वारा ज़बरदस्त विरोध हुआ। लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों और विचारों के आदान-प्रदान के आधार पर सिलसिलेवार इस की पुष्टि के बाद पहले तो वैज्ञानिकों के छोटे संसार में इस का प्रचार-प्रसार हुआ और फिर धीरे-धीरे इस परिकल्पना ने व्यापक समाज में भी अपनी जगह बना ली। हम अपनी परिकल्पनाओं को दूसरों के साथ भी साझा करते हैं और उन के विचारों को अपनी नयी परिकल्पनाओ में सम्मिलित करते हैं – यह वैचारिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया है। इस प्रकार, ज्ञान के विकास की प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया भी है।
वैज्ञानिक पद्धति और मानव-यात्रा में उस की भूमिका :
हमारे चेतन-अचेतन मन में चलने वाली जिस प्रक्रिया का वर्णन हम ने किया है, वह स्वाभाविक तौर पर, अनौपचारिक ढंग से, अनायास ही हमारे मन-मस्तिष्क में चल रही होती है। यह सब करते हुए हम शायद इस बात से अनजान होते हैं कि असल में तो यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया ही है। वैज्ञानिक प्रक्रिया, सोचने समझने की वह विधि है जिस में हम किसी भी घटना और उस के सम्भावित कारणों में वह सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिस से उस घटना की व्याख्या की जा सके। ये सम्भावित कारण इस भौतिक़ संसार में ही विद्यमान होते हैं, किसी अलौकिक शक्ति के प्रभावस्वरूप नहीं। अलौकिक शक्ति में विश्वास आस्था का प्रश्न है और विज्ञान प्रमाण के बिना आस्था को स्वीकार नहीं करता। प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए प्रयोग की जाने वाली इस विधि को हम वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हैं।
विज्ञान की मूलभूत मान्यता है कि प्रकृति कुछ विशेष नियमों के अनुसार चलती है और इन नियमों को वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से समझा जा सकता है। विज्ञान की उपरोक्त मान्यता के कारण मनुष्य प्रकृति के नियमों तक पहुँचने और उन्हें समझने के लिए यत्नशील रहता है। प्रकृति के नियम ऐसे नियम नहीं हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा बदला जा सके – वे अपरिवर्तनीय हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम आज से एक लाख साल पहले भी वैध नियम था और आज भी है। दूसरी ओर, सामाजिक नियम मानव स्वभाव और सामाजिक संरचना का परिणाम हैं और ये नियम समय तथा स्थान से प्रभावित होते हैं। हम मानव इतिहास के पिछले दो हज़ार सालों पर ही नज़र डालें तो पाएँगे कि सब से पहले समाज कबीलों में बँटा हुआ था, उस समाज के अपने नियम थे। उस के बाद दास प्रथा आयी, फिर सामन्तवाद आया और अब पूंजीवाद का ज़माना है। इन सभी समाज-व्यवस्थाओं के नियम अलग-अलग थे। इस तरह से समाज के नियमों में समाज-व्यवस्था के साथ-साथ परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन प्रकृति के नियमों में परिवर्तन न के बराबर होते हैं।
अपनी जिज्ञासा, सृजनात्मकता और श्रम की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश में दख़ल देता रहा है और ख़ुद को भी बदलता रहा है। मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचने की इच्छा की पूर्ति में, वैज्ञानिक पद्धति की मदद से वह अपने प्राप्त अनुभवों को संचित कर के और अधिक अध्ययन से अपनी समझ का लगातार विकास करता रहता है। इस लिए यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि बहुत हद तक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए ही ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति के इस पड़ाव तक पहुँचा है। मानव इतिहास के पिछले तीन सौ सालों में विज्ञान और तकनीक के विकास पर नज़र डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है। इन्सान की अवलोकन की क्षमता, उस की जिज्ञासा और उसे सन्तुष्ट करने के लिए प्रश्नों के उत्तर ढूँढने की इच्छा ने जब उसे भाप इंजन और बिजली के अविष्कार तक पहुँचाया तो दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई। फिर कई नए अविष्कार हुए, हवाई जहाज़ बने, संचार-व्यवस्था बनी, कम्प्यूटर-क्रांति आई और अब आर्टिफ़िशल इंटेलिजेन्स का विकास हो रहा है। हम चाँद तक पहुँच गए हैं और दूसरे उपग्रहों पर पहुँचने के यत्न जारी हैं।
लेकिन ध्यान इस ओर भी देना होगा कि विज्ञान और तकनीक का विकास तथा उपयोग केवल समाज के विकास के लिए ही नहीं, विनाशकारी कामों के लिए भी हुआ। एटम बम का विकास हुआ और अनेक अन्य घातक हथियारों का भी विकास हो गया है जिन से दुनिया पर जीवन को कुछ घण्टों में ही नष्ट किया जा सकता है।
वैज्ञानिक मानसिकता :
वैज्ञानिक पद्धति का यह पथ वैज्ञानिक मानसिकता के विकास का रास्ता है। पहली सीढ़ी अवलोकन के आधार पर सवाल-जवाब करना सीखना है। मानस पर उभरने वाले प्रश्नों का उत्तर खोजने की ओर प्रवृत्त हो कर एक इन्सान वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने की ओर बढ़ता है। वैज्ञानिक पद्धति की मदद से वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करते हुए ही हम हर विषय का अध्ययन कर पाते हैं। वैज्ञानिक मानसिकता के विकास के लिए दो अन्य तत्त्वों का होना आवश्यक है – तार्किक सोच तथा आलोचनात्मक सोच। तार्किक सोच से हमारा भाव है बिना किसी पक्षपात के, यानी निष्पक्षता के साथ, वस्तुनिष्ठ (objective) ढंग से सोचना और किसी निष्कर्ष तक पहुँचना। आलोचनात्मक सोच का अर्थ है, सभी पक्षों पर वाद-विवाद करते हुए निष्कर्ष निकालना – यानी किसी विषय के अलग-अलग पहलुओं का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुँचना। विश्लेषण तथा तर्क पर टिकी आलोचनात्मक तर्कपूर्ण सोच बौद्धिक रूप से अनुशासित प्रक्रिया है क्योंकि तर्क के आधार पर सोचने में निपुणता उच्चतर स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है – इस में सूचनाओं को केवल आत्मसात् करने की बजाए प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना, उन निष्कर्षों का विश्लेषण करना, उन की व्याख्या और मूल्यांकन करना या उन तर्कों में कमियाँ निकालना आदि शामिल है। आलोचनात्मक तर्कशील सोच वैज्ञानिक विश्लेषण तथा जाँच की आत्मा/केन्द्र-बिन्दु है और वैज्ञानिक पद्धति तर्कशील सोच को नियमनिष्ठ बनाती है। ये सब तत्व मिल कर वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने में मददगार होते हैं ।
वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न औपचारिक चरण :
लेख के प्रारम्भ में हम ने कहा था कि बहुत बार हम अपने सामान्य जीवन में वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण अनायास, अनौपचारिक ढंग से कर रहे होते हैं और हमें इस का एहसास भी नहीं होता। अब हम वैज्ञानिकों द्वारा इस के बाक़ायदा, औपचारिक, सचेत प्रयोग की व्याख्या करने जा रहे हैं।
प्रकृति और समाज में जो कुछ घट रहा है, उसे समझने के लिए वैज्ञानिक औपचारिक रूप से समुचित प्रश्न करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति अपना कर उन का उत्तर ढूँढने का प्रयत्न करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए वे उन प्रश्नों से जुड़े तथ्य इकट्ठा करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर वे एक सामान्य परिकल्पना (एक सरसरी व्याख्या) तैयार करते हैं कि शायद इस कारण से ऐसा हो रहा है या उस कारण से। इस परिकल्पना को हाइपौथिसिस (Hypothesis) कहते हैं। इस परिकल्पना की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए वे परिकल्पना पर आधारित नए तथ्य इकट्ठा करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति अपना कर उन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और परिकल्पना की सत्यता का मूल्यांकन करते हैं। परिकल्पना के मूल्यांकन (Testing of Hypothesis) की कई विधियाँ हैं। यदि परिकल्पना के मूल्यांकन पर वे पाते हैं कि कुछ तथ्य परिकल्पना के अनुरूप नहीं हैं, तो तथ्यों को ध्यान में रख कर पहली परिकल्पना में संशोधन करते हैं और एक नई परिकल्पना बनाते हैं और एक बार फिर तथ्यों के आधार पर उस का मूल्यांकन करते हैं। यदि फिर भी दूसरी परिकल्पना तथ्यों के अनुरूप नहीं है, तो उस में संशोधन कर के एक और नई परिकल्पना का मूल्यांकन करते हैं।
यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक वे उस एक परिकल्पना तक नही पहुँच जाते जो पूर्ण रूप से तथ्यों के अनुरूप हो। जो परिकल्पना पूर्ण रूप से तथ्यों के अनुरूप होती है, उसे नियम/सिद्धांत का दर्जा दे दिया जाता है। यदि बाद में नए तथ्य सामने आते हैं जो इस सिद्धांत के भी अनुरूप न हों, तो इस नियम में शोध कर नई परिकल्पना गढ़ी जाती है और इस नई परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिए दोबारा वैज्ञानिक मूल्यांकन की पद्धति का प्रयोग कर के उस की सत्यता को प्रमाणित करने का यत्न होता है। जो नियम बार-बार सत्य-सिद्ध हो और जिस का अपवाद न मिले, ऐसे नियम को ही उस समय के सर्वमान्य सिद्धांत का दर्जा दिया जाता है।
यह सम्पूर्ण प्रक्रिया बहुत ही सजग ढंग से चलती है और तर्क तथा प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए बहुत ही गहन शोध पर आधारित होती है। फिर भी, विज्ञान के निष्कर्ष हमेशा अस्थाई रहते हैं क्योंकि शोध आधारित नए तथ्य उद्घाटित होने पर पुराने सिद्धांत के स्थान पर नया सिद्धांत अस्तित्व में आता है। विज्ञान और वैज्ञानिकों के औपचारिक संसार में इसी सर्वमान्य पद्धति को एक प्रयोगसिद्ध वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। प्रकृति-विज्ञानियों और समाजशास्त्रियों द्वारा समय के साथ-साथ प्रश्नों की विषय-वस्तु और स्वभाव के अनुरूप औपचारिक विश्लेषण के लिए अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किया गया है।
विज्ञान के इतिहास पर नज़र डालें तो हम एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। वैज्ञानिक आइज़क न्यूटन ने सेब को पेड़ से नीचे गिरते देखा तो उस ने ख़ुद से प्रश्न किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है? फिर उस का ध्यान इस ओर गया कि अन्य भारी वस्तुएँ भी ऊँचाई से नीचे गिरती हैं। इन तथ्यों के आधार पर उस ने परिकल्पना गढ़ी कि पृथ्वी में चीज़ों को नीचे खींचने की कोई शक्ति है, जिसे उस ने गुरुत्व-शक्ति कहा और फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत करीब 200 साल तक वैज्ञानिक चिंतन पर हावी रहे। फिर बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में वैज्ञानिक आइन्स्टाइन ने देखा कि कुछ घटनाओं की व्याख्या न्यूटन के नियम से नहीं हो पाती तो उस ने न्यूटन के नियम का आगे विकास कर के सापेक्षता का सिद्धांत (Theory of Relativity) प्रतिपादित किया। आइन्स्टाइन ने अपने समय में संज्ञान में आए ताज़ा तथ्यों के आधार पर नए सिरे से परिकल्पना की और इस नई परिकल्पना के आधार पर यह सिद्धांत अस्तित्व में आया। इसी प्रकार विज्ञान के सभी नियमों का विकास हुआ – जब किसी एक युग में प्रतिपादित सिद्धांतों की सीमाएँ नज़र में आईं तो नई परिकल्पनाओं पर काम कर के उन सिद्धांतों से आगे जा कर नए सिद्धांत अस्तित्व में आते रहे।
देखने में आता है कि कई बार लोग मिथकों को भी सिद्धांत या थिअरी का दर्जा देने की कोशिश करते हैं लेकिन यह ग़लत है। मिथकों का कोई भौतिक या वैज्ञानिक आधार नहीं होता – मिथकों को तो कल्पना तथा अलौकिक शक्तियों में आस्था के आधार पर गढ़ा जाता है। पौराणिक कहानी कि शिव जी ने गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया, एक काल्पनिक कहानी है क्योंकि इस कहानी का कोई प्रमाण नहीं है और न ही वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा किया जा सकता है।
यदि किसी व्यक्ति की सोच तर्कशील तथा विश्लेषणात्मक है और वह बिना किसी जड़बद्ध आस्था पर यकीन किए वैज्ञानिक पद्धति को अपना कर समस्याओं के समाधान निकालता है, तो इस प्रकार की सोच को हम वैज्ञानिक मानसिकता से लैस सोच कह सकते हैं। तर्कशील होना तथा सभी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर चलना वैज्ञानिक मानसिकता के मूल तत्त्व हैं। वैज्ञानिक मानसिकता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वैज्ञानिक मानसिकता के साथ-साथ व्यक्ति की सोच में उच्चतम स्तर की मानवीय नैतिकता का समावेश भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर भयानक परिणाम निकल सकते हैं। एटमी शक्ति का उपयोग बिजली बनाने के लिए हो या एटम बम बनाने के लिए? समाज के लिए स्वच्छ वैज्ञानिक मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी सोच-समझ को मानव जाति और पूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए उपयोग करेगा।
वैज्ञानिक मानसिकता से लैस सोच = तर्कशील सोच + वैज्ञानिक पद्धति अपना कर प्रश्नों का उत्तर ढूँढना + उच्च मानवीय नैतिकता
जब एक व्यक्ति प्रायः सभी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति तथा तर्कशीलता का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति को वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति कह दिया जाता है। चुनौती यह है कि मानवीय मूल्यों और समग्र रूप से वैज्ञानिक मानसिकता से लैस सोच को कैसे विकसित किया जाए?
वैज्ञानिक मानसिकता का विकास कैसे हो?
केवल तर्कशील सोच का होना ही काफ़ी नहीं है जब कि इस के बिना वैज्ञानिक पद्धति के ज़रिए वैज्ञानिक सोच तक पहुँचना भी सम्भव नहीं है। चुनौतिपूर्ण समस्या यह है कि सोच को तर्कशील कैसे बनाया जाए और तर्कशील सोच को वैज्ञानिक सोच में कैसे बदला जाए?
वैज्ञानिक मानसिकता के विकास की दिशा क्या हो, यह सामाजिक संरचनाओं पर भी बहुत निर्भर करता है। इस लिए ज्ञान-विज्ञान तथा सामाजिक संरचनाओं के द्वंद्व को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास वैज्ञानिक सोच का सब से बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। अंधविश्वास आस्था और अज्ञानता से पैदा होता है। आशंका और अनिश्चितता इसे परिपक्व करते हैं। अगर मैं किसी के साथ चर्चा के दौरान कहता हूँ, “चलो आप की बात मान लेते हैं”, तो इस का अर्थ है कि मैंने खोज करने की भावना को त्याग दिया है और किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान या आस्था तक स्वयं को सीमित कर लिया है। चुप हो जाना एक बात है और उस पर आस्था से विश्वास कर लेना दूसरी बात है। प्रश्न खड़े करना, संदेह प्रकट करना और जानने की इच्छा रखना एक स्वस्थ सोच है। लेकिन किसी की बात या कथन पर विश्वास कर लेना प्रायः व्यक्ति के लिए सुविधाजनक और सहज होता है। दूसरी ओर, वैज्ञानिक सोच विकसित करना कठिन और चुनौतिपूर्ण है क्योंकि सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूँढना एक कठिन कार्य है और कई बार यह अव्यावहारिक भी हो जाता है। लेकिन किसी कथन पर आस्था बना लेना हानिकारक सिद्ध हो सकता, इस लिए उस कथन का तथ्यात्मक मूल्यांकन तो हमें हमेशा करना चाहिए। वैज्ञानिक मानसिकता वाला व्यक्ति किसी कथन को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करेगा और उस कथन का कम से कम मूल्यांकन तो करेगा ही।
विश्वास तथा आस्था की जकड़न बहुत मज़बूत होती है। इन की जड़ें मानव मस्तिष्क में बहुत गहरी जमी होती हैं। इसलिए हर स्थान पर हर प्रकार के व्यक्तियों के दिमाग़ में अंधविश्वास के बादल कम या अधिक गहरे आवश्यक रूप में पाए जाते हैं। चुनौती यह है कि हम विश्वास और अंधविश्वास के दायरों से बाहर निकल कर वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने की ओर बढ़ें – सरल पथ की बजाए कठिन पथ पर चलने को तैयार हों, क्योंकि तभी हम प्रकाश के पथ पर अग्रसर होंगे। जैसे-जैसे विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता का प्रकाश फैलता जाता है, अंधविश्वास का कोहरा छटता जाता है। लेकिन वैज्ञानिक मानसिकता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ता है।
सारतत्त्व : जैसा कि हम ने लेख के शुरू में कहा है, हर व्यक्ति में जानने की जिज्ञासा प्राकृतिक रूप से होती है। हर व्यक्ति प्रायः जिज्ञासा से उत्पन्न हुए प्रश्नों का उत्तर ढूँढने का यत्न करता है। जिज्ञासा की सन्तुष्टि के लिए प्रश्नों के उत्तर तलाशने की इच्छा तर्कशील मानसिकता के विकास का पहला क़दम है। तर्क के आधार पर ही एक व्यक्ति सम्भावित उत्तर की परिकल्पना करता है और वैज्ञानिक पद्धति की ओर बढ़ पाता है। तर्कशील हो कर वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की ओर अग्रसर होना ही वैज्ञानिक मानसिकता के विकास की कुंजी है। यह भी तय है कि वैज्ञानिक मानसिकता का निर्माण लम्बे समय तक सचेत प्रयत्न से ही किया जा सकता है।
अपनी बात का अन्त इस कथन से करना उपयुक्त होगा जो हमारे विषय से भी जा जुड़ता है:
“किसी बात पर केवल इसीलिए विश्वास न करो कि आप ने ऐसा सुना है। केवल इस लिए भी विश्वास न करो कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। विश्वास इस लिए भी न करो कि हमारे सम्मानित बड़े एवं गुरु कह रहे हैं। सदियों से चली आ रही परम्पराओं के नाते भी विश्वास न करो। परीक्षण एवं विश्लेषण के बाद जब आप को लगे कि वह तर्क-विवेक पर खरी है और यह सभी के हित में है, तभी इसे मानो और इस पर चलो।”
यह कथन वैज्ञानिक मानसिकता के विकास की महत्वपूर्ण प्ररेणा देता है। आइए, हम चेतन मन से अपनी सोच को वैज्ञानिक बनाएँ और अपने विवेक का विस्तार करें!
(लेखक प्रो. रमणीक मोहन, प्रो. राजेंद्र चौधरी, प्रिंसिपल वेदप्रिय और प्रो. प्रमोद गौरी के सुझावों तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त प्रकट करता है।)
– प्रोफ़ेसर सुरेंद्र कुमार
माल्कम अदिसेशीयह चेयर प्रोफ़ेसर, इन्स्टिट्यूट ऑव सोशल साइंसिज़, नई दिल्ली।
भूतपूर्व प्रोफ़ेसर (अर्थशास्त्र) और डीन, शैक्षणिक मामले, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
e-mail id: ksurin@rediffmail.com, M: 8005492943