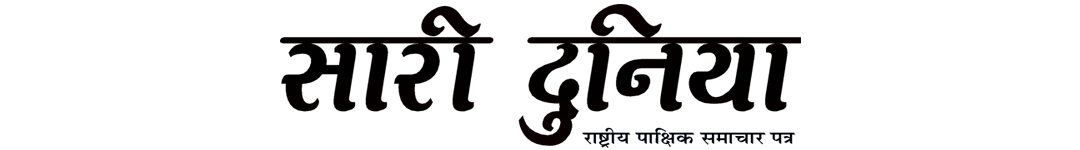बंटवारा जो बांट न सका
मूल अंग्रेज़ी: सलमान रशीद
अनुवाद: रमणीक मोहन
‘सरहद पार से’ कॉलम में आप ने सलमान रशीद के लेख पढ़े हैं जिन में वे भारत और पाकिस्तान की साझा विरासत की बात करते हैं – ख़ास तौर से वे लेख जिन में हमें सर गंगा राम के हवाले से बहुत कुछ पढ़ने को मिला। इस बार जो लेख आप पढ़ेंगे वह सलमान रशीद साहब की आप-बीती है।
यह 2014 में पुणे में हुई एक कॉन्फ़रेंस में उन द्वारा रखी गई बात के एक हिस्से का अंग्रेज़ी से अनुवाद है। यह एक ऐसी आप-बीती है जिस से हमें मालूम होता है कि उन परिवारों पर क्या बीती जो बंटवारे के वक़्त 1947 में मार-काट का शिकार हुए या जो मार-काट करने में शामिल रहे। यह भी अन्दाज़ा होता है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों ने बंटवारा होने से क्या खोया और क्या पाया। और इसे पढ़ते हुए हमें यह भी एहसास होगा कि इस बंटवारे के बावजूद हम किस तरह उस से ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं।
2017 में सलमान रशीद की विस्तृत आप-बीती अंग्रेज़ी में एक किताब के रूप में छपी – ‘अ टाइम ऑफ़ मैड्नेस: अ मेम्वा: ऑफ़ पार्टिशन’ (A Time of Madness : A Memoir of Partition) ।
1950 के दशक में जब मैं बड़ा हो रहा था, और उस के बाद भी, मैंने अपने वालिद या उन के दो बहन-भाई को कभी भी बंटवारे के ख़ौफ़नाक वक़्त के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। एक बार भी संयुक्त भारत में बीते उन के बचपन, स्कूल या फिर गाँव उग्घी और रेल्वे रोड, जालन्धर के अपने घर का ज़िक्र नहीं हुआ था। ऐसा लगता था जैसे बीते वक़्त को एक काली चादर ने ओढ़ रखा हो। मगर एक बच्चा होते हुए भी मैं उस ग़म और तकलीफ़ को महसूस कर सकता था जो मेरी बुआ की रूह को हरदम सालता था। मुझे महसूस होता था कि जैसे वे उदासी की एक हल्की सी धुंध में लिपटी रहती हों।
1985 में मेरी वालिदा के एक भाई कुछ दिनों के लिए जालन्धर गए तो हमारे घर की एक तस्वीर के साथ लौटे। वो तस्वीर सब ने देखी। मगर इस के बाद भी यादों की कोई बाढ़ नहीं आई और न ही बंटवारे से पहले के वक़्त के बारे में कोई बातचीत हुई। अजीब बात ये भी थी कि भारत से लौट कर आए इस रिश्तेदार ने यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि परिवार के लोग बंटवारे के समय कैसे मारे गए थे।
मार्च 2008 में 56 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िन्दगी में पहली बार भारत में अपने घर तक का सफ़र तय किया। अपने साथ मैं जालन्धर में रेल्वे रोड पर अपने घर की एक बड़ी तस्वीर ले कर गया था। दोस्तों को दिखाने पर जानकारी मिली कि यह भगत सिंह चौक पर है। वहाँ पहुँचा तो पहली नज़र में ही मैंने घर को पहचान लिया। सड़क की तरफ़ खुलने वाली दुकानों में एक नौजवान सिख की हार्डवेयर की दुकान थी। इक़बाल सिंह के माता-पिता सियालकोट से यहाँ आए थे। इक़बाल ने गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। काउंटर के इस ओर बैठा मैं केरीब एक घण्टे तक सड़क पर आते-जाते लोगों को देखता रहा – यही वो गलियाँ और सड़क थी जिन पर कभी मेरे परिवार के लोग भी चलते-फिरते थे।
अचानक इक़बाल ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और मुझ से पूछा, “क्या आप के दादा डॉक्टर थे?” मैंने हाँ में जवाब दिया तो वो बोला कि उस ने पूरा क़िस्सा सुन रखा है। थोड़ा सोचने के बाद उस ने कहा कि पूरी दास्तान उस ने बड़ी उम्र के अपने एक ग्राहक से सुनी थी। मैंने उस शख़्स से मिलवाने की बात कही, मगर इक़बाल को याद नहीं आ रहा था कि वो था कौन। लम्बी कहानी को मुख़्तसर करूँ तो मेरे वीज़ा की मियाद ख़त्म होने से बस एक दिन पहले उसे याद आया। सच तो ये है कि तब तक मुझे यह भी लगने लगा था कि इक़बाल को शायद इस बात का डर था कि मैं कहीं बरसों पहले की उन घटनाओं के चश्मदीद गवाह को मिलने पर बिफर कर हिंसक न हो जाऊँ – मुमकिन यह भी था कि वो शख़्स ख़ुद उस मारकाट को अंजाम देने वालों में से एक हो। मुझे इक़बाल को तसल्ली देनी पड़ी कि मेरी तरफ़ से ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर असल बात तो यही थी कि उसे याद नहीं आ रहा था कि वो पूरा क़िस्सा उसे किस ने सुनाया था।
आख़िरकार महिन्दर जी को मैं 28 मार्च 2008 को मिल पाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पहले तो मुझे मेरे दादा के घर ले कर गए। मैं वहाँ कुछ लम्हे अकेले ख़ुद के साथ गुज़ारना चाहता था। मगर अब वहाँ पर रहने वाली एक बदमिज़ाज औरत मुझे ये लम्हे देने को भी तैयार न थी। उस के बाद महिन्दर जी मुझे कृष्ण गली में ले गए। मकान के बाहर को खुलते एक दरवाज़े की ओर इशारा करते हुए बताने लगे कि किस तरह हमारा नौकर ईदू अपने दो साल के बच्चे को गोद में उठाए, उस दरवाज़े में से तीर की तरह निकला था। ये गली ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी वाली गली थी। बलवाइयों की एक भीड़ इसी तरफ़ आ रही थी और ईदू उस भीड़ के शोर को सुन कर बुरी तरह घबरा गया था।
“उस बेवक़ूफ़ तंगदिल ने उसे देख लिया था और उस पर हमला बोल दिया”, महिन्दर जी बोले। ईदू को बाज़ू वाली गली में चोपड़ा परिवार के मकान में तेज़ी से घुसते हुए देखा गया, जहाँ महिन्दर जी भी रहते थे। भीड़ उस के पीछे भागी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यह पूरी बात किसी ऐसे शख़्स से सुन रहा हूँ जो उन वाक़िआत का चश्मदीद गवाह रहा था। मेरे दिमाग़ में सवाल आया कि वे उस हिंसक भीड़ का हिस्सा कैसे हो सकते थे जब कि उस वक़्त वे महज़ 13 साल के थे? मैंने महिन्दर जी की बात को बीच में रोकते हुए यह बात पूछ ही ली।
महिन्दर जी खड़े हो गए और मुझे घूर कर देखने लगे। “आप मेरी बात नहीं सुन रहे!” वे कुछ ग़ुस्से के से लहजे में बोले। “मैं अपने पिता की बात कर रहा हूँ!” और तब मुझे एहसास हुआ कि वे अपने वालिद को बेवक़ूफ़ और तंगदिल इन्सान कह रहे थे।
चोपड़ा परिवार के घर के अन्दर महिन्दर जी ने मुझे वो सीढ़ियाँ दिखाईं जिन को फलाँगता हुआ ईदू अपने बच्चे को गोद में लिए दौड़ता चला गया था और सीनियर सहगल लपकता हुआ उस का पीछा कर रहा था। फिर वे मुझे उस कमरे में ले गए जिस में मेरे परिवार के लोग एक दूसरे के साथ सट कर इकट्टा बैठे हुए होंगे, और उन का कलेजा उन के मुँह को आ रहा होगा और वे उम्मीद कर रहे होंगे कि वे किसी तरह बच जाएँगे, उन्हें बख़्श दिया जाएगा। मेरे बार-बार पूछने पर महिन्दर जी ने बताया कि मेरे दादा को सिर में गोली मारी गई थी और बाक़ियों को तलवारों और चाकुओं से मौत के घाट उतार दिया गया था।
मेरी बुआ जवान थीं। सब से छोटी अभी हाल ही में सोलन से आई थी – वो अठारह बरस की होने को थी। मेरी उस से बड़ी बुआ और दस साल बड़ी थी। हो सकता है कि उन में से एक, या शायद दोनों ने धर्म-परिवर्तन ही कर लिया हो और सिख या हिंदू औरत के रूप में कहीं पर रह रही हों? काश, कि जिस परिवार को मैंने कभी न जाना था, किसी तरह उसे फिर से पा लूँ। मगर मेरे दिमाग़ में चल रही ये सब बातें सच नहीं थीं। कमरे में मौजूद सब को मार दिया गया था और ईदू को, जो सीढ़ियों पर सरपट दौड़ता हुआ छत पर पहुँचा था, छुरा घोंप कर मौत की आग़ोश में पहुँचा दिया गया था और उस के छोटे बच्चे को नीचे के आँगन में उछाल फैंका गया था।
पिछले कुछ मिनट मेरे लिए एक तेज़-रफ़्तार फ़िल्म की तरह गुज़रे थे। लेकिन बाद में, शाम को जब मैंने देश भगत यादगार हॉल के अपने कमरे में महिन्दर जी की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को बार-बार सुना, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी एक साझा विरासत है। इधर मैंने बंटवारे के बारे में कभी भी बात न करने वाले अपने परिवार से गहरा ग़म विरासत में पाया था तो उधर गुनहगार होने के बोझ की, अपराध-बोध की विरासत, महिन्दर जी के हिस्से आई थी। महिन्दर जी ने एक ऐसे पिता का अपराध-बोध पाया था जो उस पागलपन के गुज़र जाने के कुछ ही दिनों के भीतर गुनहगार होने के बोझ तले आ गए थे।
उन्हें उस भीड़ में शामिल होने का पछतावा होने लगा था। वे हमेशा – कभी-कभी आँखों में आँसू लिए – कहते थे कि डॉक्टर साहब एक अच्छे इन्सान थे और जो हुआ, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। महिन्दर जी ने बताया कि 1970 के दशक में उन की मौत के समय तक वे उस भयानक कृत्य के अपराध-बोध से छुटकारा न पा सके थे। वे उस घटनाक्रम में अपनी हिस्सेदारी के बारे में अक्सर यूँ बात करते थे जैसे अपनी आत्मा को धोना-माँजना, उसे साफ़-पाक करना चाह रहे हों।
मुझ से मिलना और बात करना महिन्दर जी के लिए भी उतना ही ज़रूरी था जितना कि मेरा उन से मिलना और बात करना। हम दोनों को ही अपने भीतर के प्रेतों को झाड़-फूँक कर निकालना था और हमें सताने वाले अपने भूतकाल से जूझना और निपटना था। आज मुझे बस यह अफ़सोस है कि महिन्दर जी के मार्च 2011 में गुज़र जाने से पहले मैं उन से एक बात नहीं पूछ पाया – क्या मुझे मिलने से पहले वे किसी ऐसे इन्सान से मिलना चाह रहे थे जिस का सम्बन्ध इतना अरसा पहले मारे गए लोगों से हो, ताकि अपनी आत्मा के दर्द को पाक-साफ़ कर के निकाल बाहर कर सकें, उस से निजात पा सकें?
मुझे अब समझ में आया कि क्यों मेरे वालिद और उन के भाई कभी भी बंटवारे का ज़िक्र नहीं करते थे और उस ग़म को भी समझ पाया जिसे मेरी बुआ पूरी उम्र जीती रही। अफ़सोस कि मैं जब हिन्दोस्तान पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे वालिद को गुज़रे तीन साल हो चुके थे और उन के भाई-बहन को गुज़रे उस से भी ज़्यादा साल। अब कोई न बचा था जिसे मैं बता पाता कि उन के प्यारों के साथ जो किया गया था, महिन्दर जी के वालिद उस के लिए शर्मिंदगी महसूस करते थे।
मैं तो बस उन लाखों में से सिर्फ़ एक हूँ जिन के पास ऐसी ही कहानियाँ सुनाने को हैं। मेरे मन में महिन्दर जी के लिए कड़वाहट और तल्ख़ी का न होना भी मुझे अनोखा या बेजोड़ नहीं बनाता। उस के बाद तीन बार मेरा भारत में आना हुआ और मैं उन से मिला। हर बार उन से तोहफ़े के साथ मिलना मेरे लिए शुक्रगुज़ारी की बात रही। उन का होना ही अपने आप में बहुत तसल्ली देता था। उन का गुज़र जाना मेरे लिए दुख की बात है क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िन्दगी के एक बड़े ख़ला को, मेरे जीवन के एक ख़ालीपन को, भरा था।
जालन्धर में मुझे नेकदिल महिन्दर जी मिले तो मेरे जद्दी गाँव उग्घी में भी मुझे ‘परिवार’ मिला। सरदार सौदागर सिंह जोसान बहुत पुराने वक़्त से हमारे नातेदार हैं, क्योंकि हम एक ही जात के हैं। उन की जवानी का एक हिस्सा लायलपुर के नज़दीक शाहकोट में बीता था। उन के वालिद फ़िरोज़पुर से एक ग़रीब किसान थे जिन्हें 1932 में नई नहरों के बीच बसे रेतीले इलाक़े में खेती लायक़ ज़मीन मुहैया करवाई गई थी। करीब-करीब दो दशकों तक उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए एक ख़ुशहाल ज़िन्दगी की ख़ातिर हल जोत कर कड़ी मेहनत की थी।
लेकिन कड़ी मेहनत के ये साल अगस्त 1947 में धुँआ हो गए। सौदागर सिंह तब तेरह साल से भी कम उम्र के थे। बिना सोचे-समझे एक लकीर पंजाब की धरती और दिल को चीर कर खैंच दी गई थी। लाखों लोगों की तरह सौदागर सिंह और उन का परिवार भी उस लकीर के पार पूर्व की तरफ़ भाग निकलने को मजबूर हुए। क़िस्मत उन्हें उग्घी ले आई। साथ ही एक बार फिर ग़रीबी आई। जिस ज़मीन पर उन्होंने नए सिरे से काम शुरू किया, उस की मिट्टी में मेरे पूर्वजों की हड्डियाँ खाद की तरह रची-बसी थीं।
ऊँचे-लम्बे, बिना दाढ़ी के चेहरे वाले, ख़ूबसूरत बख़्शिश सिंह को जब मैं देश भगत हॉल, जालन्धर में मिला तो उन्होंने मुझे अपने गाँव घर पर आने का न्यौता दिया। 2008 में मार्च आख़िर के उस दिन के बाद से सादा पंजाबी किसानों का ये परिवार मेरे और मेरी पत्नी के लिए भी परिवार की ही तरह है। गाँव में उन के घर हम उसी तरह जाते हैं और वहीं रुकते हैं, जैसे कि उन्हें मिलने आया कोई भी रिश्तेदार। जब सौदागर सिंह 2011 में तीर्थयात्रियों के जत्थे के साथ आए तो लाहौर में जिस होस्टल में वे ठहरे थे, उस का बन्दोबस्त देखने वालों से मैंने कहा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं – किसी ने भी मेरी बात पर शक नहीं किया।
इस महान और कमाल के उपमहाद्वीप में रहने वाले हम लोगों को अपने ज़ख़्म भरने हैं तो हमें एक दूसरे से मिलने के मौक़े बढ़ाने होंगे। और ये ज़ख़्म तब ही भरेंगे जब हम एक-दूसरे को जानेंगे। यह बात पंजाब के लोगों पर तो और भी ज़्यादा लागू होती है क्योंकि उन्होंने ही बंटवारे के दौरान सब से ज़्यादा कष्ट झेला था। हमारे लिए एक दूसरे को मिलना इस लिए ज़रूरी है कि हम देख पाएँ कि हम में से किसी की भी चमड़ी हरी नहीं है, न ही हमारे सिरों पर सींग हैं – हम सब इन्सान ही हैं, और भाई-बंधु हैं। बहुत ख़ून बहाया जा चुका है। अब तो इसे रोकें!
पाकिस्तान के गिलगिट-बाल्टिस्तान इलाक़े के लोग एक वक़्त पर पन्दरह दिनों के लिए चीन के ज़िन्जियाँग सूबे के किसी भी भाग में घूम सकते हैं और इस के लिए उन्हें गिलगिट के डेप्युटी कमिश्नर की ओर से जारी किए गए, आवाजाही के लिए एक पत्र की ज़रूरत होती है, बस। यही बात ईरान की सरहद पर बलोचिस्तान के ज़िलों पर भी लागू होती है। जहाँ तक दर्रा ख़ैबर में तोरख़म पर स्थित सरहद की बात है, उसे तो एक मज़ाक़ ही समझिए। सरहद के खुलने पर दोनों तरफ़ के लोग इस तरह इधर से उधर और उधर से इधर आ-जा रहे होते हैं जैसे कि यह जर्मनी और हॉलैण्ड के बीच आवाजाही का मुक़ाम हो।
अगर हम तीन सरहदों पर यह कर सकते हैं तो वाघा और अटारी पर क्यों नहीं? रैड्क्लिफ़ रेखा के दोनों तरफ़ पंजाब के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि हमें बंटवारे के करीब 70 साल बाद भी यह झेलना पड़ रहा है? असल में तो ये बेइन्साफ़ी पंजाब ही नहीं, समूचे उपमहाद्वीप के लिए सच और प्रासंगिक है। दोनों तरफ़ सरहद के आर-पार सफ़र करने के लिए बहुत कम पाबंदियाँ होनी चाहिएँ। युवा वर्ग पर ख़ास ध्यान केन्द्रित करते हुए फ़ौरन सांस्कृतिक आदान-प्रदान की ज़रूरत है। बेहतर यही है कि इस नक़ली बंटवारे के आर-पार लोग एक दूसरे को क़ुबूल करते हुए बड़े हों।
हम भारत के लोग नफ़रत से नहीं बने हैं। मैं यह बात इतिहास की रौशनी में कह रहा हूँ। सिकन्दर के प्रमुख इतिहासकार एरिअन (Arrian) ने सिकन्दर के काल का इतिहास उस के तीन सदियों बाद अपनी पुस्तक ‘इण्डिका’ (Indika) में दर्ज किया था (यह उस के समय में मौजूद और उपलब्ध उन स्रोतों पर आधारित है जो अब अस्तित्व में नहीं हैं)। एरिअन इस बात को दर्ज करता है कि भारतीयों में इन्साफ़ का बड़ा जज़्बा था और वे अन्य लोगों पर हमला नहीं करते थे, और न ही बाहर से उन पर हमले होते थे। सिकन्दर से सम्बद्ध अन्य इतिहासकार बताते हैं कि तक्षशिला एक स्वर्ग की तरह था जहाँ चोरी और धोखेबाज़ी नाम की चीज़ नहीं थी और तीन धर्म सह-अस्तित्व में मौजूद थे।
सिन्धु घाटी के बड़े शहरों की बात करें तो पाकिस्तान में इन के खण्डहरों के विस्तृत अध्ययन और खोजबीन से न तो हड़प्पा में और न ही मोहन्जोदड़ो में सुरक्षा के लिए दीवारों के होने का कोई सबूत मिलता है। दीवारें सिर्फ़ शहरों की अलग पहचान के लिए, उन की सीमाओं की निशानदेही के लिए, थीं। बड़े द्वार आने-जाने वालों की हलचल को नियंत्रित करने के लिए थे, और किसी भी तरह के सुरक्षा के बन्दोबस्त नहीं थे। इन दोनों में से किसी भी शहर में राजाओं और योद्धाओं के लिए बनाए गए स्मारकों के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। न ही युद्ध के यशगान और शत्रुओं को पराजित किए जाने के कोई निशान मिले हैं।
इस उप-महाद्वीप के लोग अपने सारतत्व में प्राचीन संसार के सूफ़ी थे। इस देश ने शांति के सच्चे धर्म, यानी बौद्ध धर्म, को जन्म दिया। इतिहास के रास्ते में कहीं हम ने उस आत्मा को खो दिया जिस ने हमें मानवीय बनाया था। अब वक़्त है कि हम ने जो खो दिया था, उसे फिर से हासिल करें। वक़्त है कि हम दुशमनी और जंग को पीछे छोड़ कर वो बनें जिस के लिए हम यूनानियों में विख्यात थे।