‘बम्बा मेल’ यहाँ भी आती थी
मूल अंग्रेज़ी: सलमान रशीद
अनुवाद: रमणीक मोहन
(सलमान रशीद मूल रूप से यात्रा-वृत्तांतों के लेखक हैं और उन के इन वृत्तांतों की कई पुस्तकें छप चुकी हैं। यह लेख उन की किताब ‘सी मॉन्स्टर्ज़ एण्ड द सन गॉड : ट्रैवल्ज़ इन पाकिस्तान’ से लिए गए मूल अंग्रेज़ी लेख ‘द बम्बा मेल’ कॉल्ड हेयर् का अनुवाद है, जिसे ‘सारी दुनिया’ में छापे जाने के लिए उन्होंने बख़ुशी इजाज़त दी है।
कैसा रहा होगा 1947 से पहले का वह समय जब रेलगाड़ियाँ आज के भारत और पाकिस्तान वाले इलाक़ों के आर-पार सरहद के भय के बिना चलती थीं? क्या हुआ होगा उन रेल्वे स्टेशनों का जहाँ तक अब वो ट्रेनें नहीं जातीं? क्यों नहीं हमारे दोनों मुल्कों के बीच ट्रेन का सफ़र पहले की तरह हो सकता? ऐसे ही सवाल ज़ेहन में छोड़ जाता है यह वृत्तांत जो शुरू होता है बंटवारे से पहले के वक़्त के साथ और ख़त्म होता है एक ख़्वाब पे आ कर।)
एक वक़्त था जब नई सरहद की लकीर धरती पर नहीं खैंची गई थी और पाकिस्तान ने अभी जन्म नहीं लिया था। यह वो वक़्त था जब कराची से कोलकता तक की ट्रेनें दिल्ली से होते हुए निकलती थीं। ये बहावलपुर पहुँचने पर आज की हमारी ‘मेन लाइन’ को पीछे छोड़ कर उत्तर-पूर्व की तरफ़ मुड़ जाती थीं। रेगिस्तान को पार करते हुए बहावलनगर और फिर आगे मण्डी सादिक़गंज के जंक्शन पर पहुँचती थीं। यहाँ से वे या तो अमरूका से होते हुए फ़ाज़िल्का तक जाती थीं, या फिर पूर्व की ओर भटिण्डा, जो बंटवारे से पहले के भारत के सब से व्यस्त रेल्वे जंक्शनों में से एक था। भटिण्डा से यात्री कई ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन पकड़ कर किसी भी दिशा में जा सकते थे।
अविभाजित भारत में भटिण्डा वाला दायरा पेशावर और कोलकता के बीच चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था। लाहौर और जालन्धर से होते हुए दिल्ली तक की सीधी लाइन के मुक़ाबले यह ज़्यादा लम्बा और थकाऊ-उबाऊ रूट था। इसी वजह से इस के लिए ‘वाया भटिण्डा’ की शब्दावली आम प्रयोग में आ गई, जिस का इस्तेमाल घुमावदार तरीक़े से कही जाने वाली बात या किसी बेमतलब और चक्करदार यात्रा के लिए किया जाने लगा। ‘वाया भटिण्डा’ 1970 के दशक तक इस्तेमाल होता रहा। फिर चुपचाप ये जैसे गुमनामी में चला गया, शायद इस वजह से कि उस पीढ़ी के लोगों की तादाद बहुत घट गई थी जो इस के अर्थ और महत्व को समझते थे।
मगर फिर वो लकीर खैंच दी गई और भारत का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान एक अलग मुल्क की हैसीयत से अस्तित्व में आ गया। सफ़र के प्राचीन रूटों पर जो शहर और नगर कभी सक्रिय केन्द्र रहे थे, अचानक दो पड़ोसियों के बैरी किनारों पर आ गए। अब वे ऐसे स्थान बन गए जिन से हो कर यात्री नहीं गुज़रते थे। ये सरहद के ऐसे शहर बन गए जहाँ लोग अमूमन नहीं ही जाते थे – कोई ज़रूरी काम निकल आने पर ही जाते थे : जो पहले मध्य-बिन्दु थे, वे अब यात्राओं के अन्त-स्थान बन गए। इसी तरह महान ट्रंक रेल्वे पर स्थित यात्रा के महत्वपूर्ण बिन्दु उन रेलगाड़ियों के लिए अंतिम स्टेशन बन गए जो कभी पूरी शान के साथ पंजाब के दूर तक फैले मैदानी इलाक़ों में से हो कर गुज़रती थीं।
वक़्त गुज़रने के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में परिपक्व होने की बजाए अत्यधिक भ्रमग्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान के आम लोगों के लिए सरहद पर स्थित इन नगरों की यात्रा आज़ादी से करना मुश्किल हो गया है – इस डर की वजह से कि उन्हें उन ख़ौफ़नाक ख़ुफिया एजेंसियों द्वारा तंग किया जाएगा जो आज भी दो सौ साल पहले के युग में जी रही हैं जब अभी कैमरा की ईजाद नहीं हुई थी और हर यात्री लाज़िमी तौर पर जासूस हुआ करता था। जासूसी उपग्रहों के बारे में तो जैसे इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। इन्हें अब भी लगता है कि कहीं पर स्थापित ‘अत्यंत महत्वपूर्ण’ संयंत्रों की तस्वीरें खैंचने और उन का नक़्शा तैयार करने के लिए तो जासूसों को वहीं जाना होगा। नतीजा यह, कि अगर मेरे दोस्त काशिफ़ नून बहावलपुर से न होते तो मैं भी शायद भारत की सरहद पर स्थित मण्डी सादिक़गंज के उजाड़-सुनसान रेल्वे स्टेशन तक न जाता।
इस दौरान पाकिस्तान में रेल्वे का वैसे भी कोई अच्छा हाल नहीं था। एक के बाद दूसरी सरकार ने इसे सब से कम प्राथमिकता पर रखा और इसी का नतीजा था कि 1970 का दशक आते-आते, कभी कार्यकुशल रही ये विशाल मशीनरी अब चरमराने लगी थी। उधर पड़ोसी भारत तेज़ ट्रेनों और नई लाइनों के दम पर आगे निकल रहा था और इधर हम ब्रिटिश राज से विरासत में मिले रेल्वे के बड़े सेक्शन बन्द कर रहे थे। लेकिन दुनिया में कोई भी रेल्वे सवारियों के दम पर पैसा नहीं कमाती – कमाई तो माल को इधर से उधर लाने-ले जाने से होती है। इस लिए रेल्वे के ताबूत में आख़री कील तब ठोका गया जब 1970 की दहाई में नैश्नल लॉजिस्टिक सेल की स्थापना की गई।
बड़ी तादाद में लॉरियों और ट्रेलर-ट्रकों का असल मतलब था कि कुछ ताक़तवर लोगों की जेबें बड़े-बड़े कमिशनों से भरने लगीं। इस बात की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया कि पाकिस्तान जैसे लम्बे और कम चौड़ाई के देश में सड़क की बजाए रेल से माल का लाना-ले जाना ज़्यादा सही और बेहतर था। मुल्क भर की सड़कों पर सैंकड़ों लॉरियों से निकलते धुएँ से पर्यावरण को होने वाले नुक़्सान के बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया जब कि एक लोकोमोटिव सौ से ज़्यादा माल-वैगनों को खैंच सकता है। न ही पहले से टूटी सड़कों को होने वाले नुक़्सान के बारे में कुछ सोचा गया। ध्यान रखा गया तो बस स्विट्ज़रलैण्ड के मोटे बैंक अकाउण्ट्स का। और इस तरह वो गर्वीली उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, जो हमें आज़ादी के वक़्त मिली थी, आज इस हाल में पहुँच गई है कि उसे फिर से ज़िन्दा करने के लिए हर तरह के अव्यावहारिक, उल्टे-सीधे तरीक़ों से कोशिश की जा रही है।
हम सुबह जल्दी ही बहावलपुर से निकल गए। बहावलनगर में हम ने काफ़ी वक़्त ज़ाया किया क्योंकि वहाँ से सादिक़गंज के लिए निकलने से पहले हम ने ज़रूरत से बड़ी और ख़ुद को अहमियत देने वाली खोजी मुहिम की शक़्ल लेना शुरू कर दिया। ख़ुद को अहमियत देने वाली इस लिए, कि अगर हम बस दो ही लोग होते तो बिना किसी मक़सद के सुनसान रेल्वे स्टेशनों पर इधर-उधर घूमते दो बन्दों को देख कर कौन उन की तरफ़ ध्यान देता! जब काशिफ़ का भाई बहावलनगर में हमारे साथ आ मिला तो उस के दो और दोस्त भी साथ हो लिए थे। काशिफ़ के भाई के साथ होने का एक फ़ायदा यह भी हुआ कि हमें एक हथियारबंद गारद भी मिल गया। हम मिंचिनाबाद के बाज़ारों में गाँव के लोगों की भीड़ वाले इलाक़ों के बीच से हो कर निकले तो पूर्व दिशा में सरहद की तरफ़ मुड़ गए। जल्द ही मैदान की धूल और गर्मी के बीच से सादिक़गंज दिखाई दिया – खजूर के पेड़ों के साथ-साथ अन्य पेड़ों से घिरे, मिट्टी की रंगत वाले मकान, एकमुश्त नज़रों के सामने आए।
रेल्वे स्टेशन नगर के बाहर था, पूर्व की ओर। क्रीम रंग की इमारत के सामने दो लड़के कोई बचकाना खेल खेल रहे थे। लेकिन हमारे हथियारबंद गारद को देख कर वो वहाँ से रफ़ू-चक्कर हो गए। ड्योढ़ी सुनसान थी। एक ही प्लैट्फ़ॉर्म था। वहाँ बस दो ही लोग मौजूद थे जिन में से एक, कुछ बड़ी उम्र का, देखने में शानदार शख़्स, एक बेंच पर बैठा कहीं दूर टकटकी लगाए देख रहा था जब कि उस के घुटने पर उस की छड़ी झुकी हुई टिकी थी। बेंच के पास ही, ज़मीन पर, जुगाली करती एक बकरी बैठी थी। दूसरा, जवान और दाढ़ी वाला शख़्स, स्टेशन- मास्टर के तालाबन्द दफ़्तर के बाहर बेंच पर बैठा था। उस के पीछे एक नोटिस लगा हुआ था कि स्टेशन-मास्टर के दफ़्तर में प्रवेश के लिए इजाज़त लेना होगी। उस के साथ ही एक और नोटिस चेतावनी दे रहा था: ‘वर्जित क्षेत्र। फ़ोटो खैंचने की इजाज़त नहीं है।’ – शायद बात पर ज़ोर देने के मक़सद से, यह सब लाल अक्षरों में लिखा हुआ था।
खुले तौर पर ख़ुद को देशभक्त न मानने वाला और इस बात का क़ायल कि सादिक़गंज के इस करीब-करीब बन्द पड़े रेल्वे-स्टेशन पर स्टेशन-मास्टर के ताला लगे दफ़्तर की तस्वीर के लिए भारत से (और शायद इज़राइल से भी) अच्छा-ख़ासा धन मिल सकता है, मैंने ग़ैर-क़ानूनी काम कर ही दिया। कोई सायरन नहीं बजे और कहीं से भी लुके-छुपे एजेण्ट मुझे गिरफ़्तार करने के लिए नहीं आ धमके।
इसी बीच हम सब को इधर-उधर घूमते, आवारगर्दी करते देख, एक बड़ी उम्र का रेल्वेमैन, जिसे रिटायर हुए तीन साल हो चुके थे, पूछताछ करने आ पहुँचा। उस ने मण्डी सादिक़गंज रेल्वे स्टेशन के यश भरे दिन देखे थे।
“कुछ ही साल पहले तक, अप और डाउन, आठ ट्रेनें यहाँ से हो कर गुज़रती थीं। तब आते तो देखते हमारे स्टेशन की रौनक़!” – उस ने बहुत ही गर्व के साथ कहा। “और यह तो बंटवारे के बाद की बात है। उस से पहले तो यह क्या ही शानदार स्टेशन था जिस का प्रताप देखते ही बनता था – और भी ज़्यादा ट्रेनें थीं तब तो।”
बंटवारे से पहले की ट्रेनों में फ़िरोज़पुर और बहावलनगर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें थीं और मण्डी सादिक़गंज से फ़िरोज़पुर को लौटने वाली ट्रेनें भी, जो बाहर के प्लैट्फ़ॉर्म पर रात को इन्तज़ार करने के बाद जाती थीं। उस ने उस जगह की तरफ़ इशारा किया जहाँ वापसी के लिए रात को उन्हें धोया-साफ़ किया जाता था। मगर इन सब में, सब से अहम तो रोज़ अप और डाउन करने वाली ‘बम्बा’ (शायद बॉम्बे?) मेल थी जो एक आंधी की तरह स्टेशन पर आती थी। उस का रुकना बस थोड़ी ही देर का होता था। फिर चिंगारियाँ उगलते पहियों, रात की चुप्पी को तोड़ती हुई चीख़ती सीटी और गरजते-गूंजते बॉयलर की आवाज़ों के साथ वो सो रहे सादिक़गंजवालों को जगाते हुए, स्टेशन से दनदनाती हुई निकलती थी। अपना माल बेचने वाले, ट्रेन के साथ-साथ दौड़ते चले जाते थे – खिड़कियों से बाहर कोनिकलते सवारियों के हाथ, कभी तो माल बेचने वालों के हाथों से मिल पाते, अकसर नहीं ही मिल पाते थे। और फिर सब शांत हो जाता था। मैं यह तो नहीं जान पाया कि बॉम्बे मेल कहाँ से शुरू होती या कहाँ जा कर ख़त्म होती थी या किस लाइन पर चलते हुए सादिक़गंज से हो कर गुज़रती थी, मगर कहानी मुझे रोमांचित करने वाली ज़रूर लगी।
किसी को स्टेशन मास्टर के दफ़्तर की चाबी लिवाने के लिए भेजा गया और हमें दफ़्तर में प्रवेश मिल गया। जैसा अमूमन होता है, दफ़्तर में दीवारों पर रजिस्टर लटके (जी हाँ, लटके) हुए थे। इन लटकते हुए रजिस्टरों में से मेरी पसन्दीदा नस्ल इस नाम से है – ‘लिस्ट ऑफ़ ऑफ़िशिअल्स इन केस ऑफ़ एक्सिडेंट टेलिग्राम्ज़’। टेबल पर मोटे पेट वाला पीतल का एक मिट्टी के तेल का लैम्प था जिस की शीशे की चिमनी टूटी हुई थी। जिस बन्दे ने हमें प्रवेश दिलवाया था (और जिस का नाम मैंने पूछा ही नहीं), उस की नज़रें पुराने ज़माने के इस लैम्प तक जाती हुई मेरी निगाह का पीछा कर रही थीं। वो बोला – “मेरे वक़्त में बिजली और पानी हुआ करता था। अब कुछ भी नहीं है और स्टेशन-मास्टर इसी लैम्प का इस्तेमाल करते हैं।” फिर मुँह-बंद हँसी के साथ बोला – “मगर वो तो तब है जब उन्हें अंधेरा पड़ने के बाद काम हो, जो कभी-कभार ही होता है।”
वो हमें बाहर ले आया। नीचे को तिरछी ढलती हुई छत वाली कोठरी में, जिस में पानी के बड़े-बड़े मटके धरे रहते थे, उर्दू में लिखे उन अल्फ़ाज़ के साथ जो सूचना दे रहे होते – ‘पीने का पानी’। फिर एक वक़्त आया जब पानी के इलेक्ट्रिक कूलर ने इन की जगह ले ली। लेकिन अब तो वो भी नहीं था और कोठरी ख़ाली थी। मण्डी सादिक़गंज के स्टेशन पर उतरने वाली गिनी-चुनी सवारियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए घर पहुँचने तक का इन्तज़ार करना पड़ेगा।
“मण्डी सादिक़गंज का तो खेल तमाम हो गया। जब स्टीम लोकोमोटिव धीरे –धीरे कम होते चले गए, तो पानी की ज़रूरत भी बहुत कम रह गई। लेकिन अब सिर्फ़ एक अप और डाउन ट्रेन के चलते, वो भी डीज़ल की, पीने के पानी का भी ध्यान नहीं रखा जाता”, शिकायतों से भरा वो शख़्स बोला। “वैसे भी, ट्रेन इतनी सुस्त-रफ़्तार है कि न के बराबर लोग ही इस का इस्तेमाल करते हैं। वो अब ज़्यादा तेज़-रफ़्तार बसों में जाते हैं। स्टेशन तो समझें कि बस बन्द ही पड़ा है।”
हमारी इल्तिजा पर पुरुषों का वेटिंग-रूम खोल दिया गया। पच्चीकारी वाला टाइलों का फ़र्श सफ़ाई मांगता था मगर बीते समय में बेहतर हालात की तस्दीक़ भी करता था। नियमित नोटिस और फर्निचर सब मौजूद थे – बेंत की सेटी, गोल मेज़ और उस के इर्द-गिर्द सीधी पीठ की कुर्सियाँ, और दो कुर्सियाँ जिन्हें सामान-सूची में ‘कुर्सी, लम्बी बाज़ू वाली’ के तौर पर दर्ज किया गया है। यह कुर्सी अधलेटी अवस्था में सोने के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
मैंने पूछा कि क्या बहावलपुर वाली इस लाइन का अंतिम स्टेशन अमरूका इस लायक़ है कि किसी को उसे देखने में दिलचस्पी हो? उस शख़्स ने बहुत ही पक्के तौर पर ‘नहीं’ कुछ इस अन्दाज़ से कहा कि इस लाइन के अंत तक पहुँचने के मक़सद से बाक़ी के बीस-एक किलोमीटर के सफ़र पर आगे चलने के लिए काशिफ़ को कहना मुझे मुनासिब नहीं लगा।
इस बात का कोई रिकॉर्ड अब मौजूद नहीं है कि मण्डी सादिक़गंज से होते हुए हिंदू मलकोट (जो इस लाइन पर अब भारत का स्टेशन है) और उस से आगे भटिण्डा के लिए यह नियमित रेल-सेवा आख़री बार कब चली। लेकिन 1947 के मध्य-अगस्त से दो महीनों के लिए सिर्फ़ रिफ़्यूजी-ट्रेनें ही यहाँ से हो कर गुज़रती थीं – कभी-कभी इन्सानों की लाशों को लादे हुए। वक़्त गुज़रता गया, भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते बदहाल होते गए और दोनों मुल्कों के बीच बेरोकटोक सफ़र का ख़्वाब ओझल होता चला गया। फिर एक वक़्त यह भी आया कि अमरूका और हिंदू मलकोट के बीच की रेल पटरी उखाड़ दी गई – शायद बढ़ती चली आ रही भारतीय सेना से बचाव और एहतियात के तौर पर। इस पटरी के उखाड़े जाने का मतलब था कि इस लाइन का अन्तर-राष्ट्रीय चरित्र समाप्त हो गया।
मण्डी सादिक़गंज की मेरी इस यात्रा के कुछ अरसा बाद मैंने दोनों कोरिया देशों के बारे में ख़बर पढ़ी कि किस तरह कड़वाहट से भरे, एक वक़्त के दो दुशमन पचास साल की मूर्खतापूर्ण आक्रामकता के बाद एक दूसरे के साथ समझौते को तैयार हो गएहैं। जैसे दिन के बाद रात का आना पक्का है, उसी तरह संसार के हमारे ख़ित्ते में भी कभी न कभी तो ऐसा ही कुछ होगा जैसा दोनों कोरियाओं के बीच हुआ है। और मैं सोचे बिना नहीं रह सकता कि जब ऐसा हो जाएगा तो क्या रेल्वे-एंजिनियर गुमनाम हिन्दू मलकोट और सादिक़गंज के बीच की रेल्वे लाइन को फिर से ज़िन्दा करने में दिलचस्पी लेंगे? यह ख़याल रह-रह कर मेरे मन में आता है। अगर वे ऐसा कर दें तो वे जोशीले रेल-यात्रियों के लिए यह भी मुमकिन कर देंगे कि वो कोलकता से शुरूआत करते हुए लंदन के विक्टोरिया स्टेशन तक के सफ़र पर निकल सकें। कितना शानदार सपना है ये! और क्या ही कमाल का सफ़र हो बनेगा वो!!
===============
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
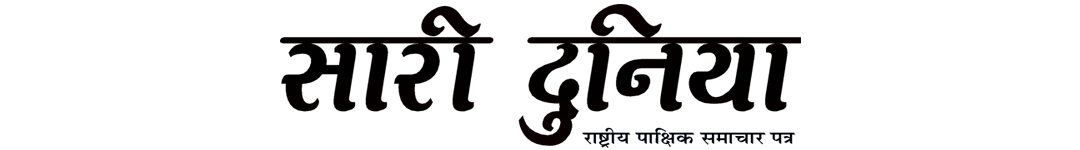

बेहद शानदार. लफ़्ज़ों के जरिए गुमनाम रास्तों की सैर का मौका मिला. शुक्रिया